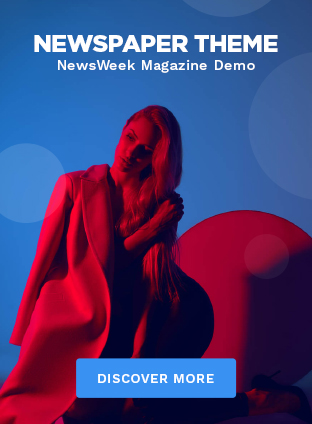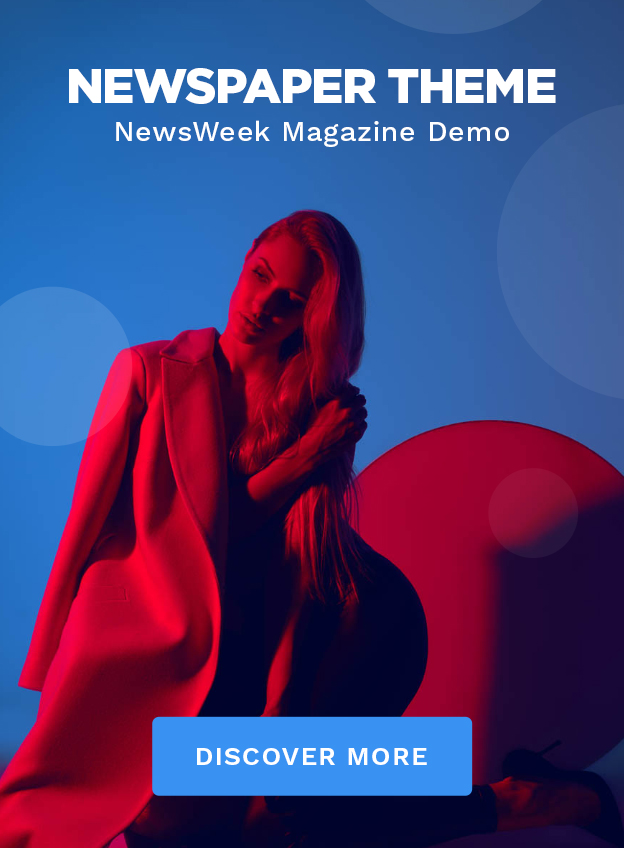डिजिटल द्वार पर दस्तक देती संवेदनाएँ, टूटते संबंधों की कहानियाँ और बदलते सामाजिक मानस का मार्मिक चित्र
— डॉ प्रियंका सौरभ
मेसेंजर के आभासी प्रांगण में कुछ अनाम आत्माएँ प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल ऐसे उतर आती हैं, मानो मेरे मन-लोक के द्वार उनकी प्रतीक्षा में ही सदैव खुले रहते हों। उनके संदेशों का प्रवाह इतना निरंतर, इतना अविरल होता है कि लगता है जैसे किसी सुदूर स्रोत से आशा की कोई अदृश्य नदी बहती चली आ रही हो। यह भी विचित्र है कि इन संदेशों के उत्तर की उन्हें तनिक भी चिंता नहीं—उनके शब्दों में एक ऐसी निस्सीम आशा झलकती है मानो दुनिया का ध्वंस भी उनसे उनकी जिजीविषा न छीन पाएगा।
जब कभी मैं मेसेंजर खोलती हूँ, तो भीतर कृत्रिम पुष्पों की रंग-बिरंगी पाँतें, कोमल उपमाओं की मधुमयी धाराएँ और शब्दों की शक्कर से लिपटी मिठास मेरी आँखों के समक्ष फैल जाती है। वह क्षण किसी अनजाने उत्सव-सा लगता है—एक ऐसा उत्सव, जिसे किसी ने बिना निमंत्रण दिए मेरे जीवन में बिखेर दिया हो। कभी-कभी मन यूँ ही सोच में डूब जाता है—क्या सचमुच कोई अजनबी नारी किसी अनदेखे- अनजाने व्यक्ति के हृदय में इतना सारा मृदु स्नेह, इतनी कोमल भावनाएँ और इतना अनुशासित आदर जगा सकता है?
परंतु इसी कोने में एक गहरी विडंबना भी खड़ी है—अपने निजी जीवन में तो जीवनसाथी के मुख से एक मधुर शब्द भी सुनने को नहीं मिलता। वहाँ तो केवल शिकायतों की काँटेदार झाड़ियाँ और उलाहनों की सूखी टहनियाँ ही पनपती हैं। कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे विवाह नामक संस्था ने दो अधूरे मनुष्यों को एक साथ बाँधकर उनसे पूर्णता की अपेक्षा कर ली हो, जबकि भीतर दोनों ही अपूर्णताओं और अनकहे दुःखों के बोझ तले दबे हों।
फिर भी, इन अनाम स्नेहदाताओं के प्रति मेरे भीतर एक विचित्र-सा आभार जन्म लेता है। शायद यह आभार किसी अपेक्षा का नहीं, बल्कि इस भाव का है कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ, बिना पहचान, बिना अपेक्षा—स्नेह देना जानते हैं। इस सत्य की मधुर अनुभूति ही हृदय में एक अदृश्य कृतज्ञता अंकित कर देती है। किन्तु मेरे अस्तित्व के भीतर इन अजनबियों के लिए किसी भी भाव—प्रेम, आकर्षण या खिंचाव—की कोई जगह नहीं। मेरे भीतर जो स्थान सुरक्षित है, वह वीतराग के विस्तृत आकाश की तरह रिक्त और शांत है।
मेरे परिचय-वलय में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो दुनिया को हँसी के उत्सव बाँटता फिरता है। वह अपनी चुटीली टिप्पणियों और सहज हास्य से लोगों के चेहरे पर मुस्कान उगा देता है, लेकिन जैसे ही वह घर के मुख्यद्वार पर पहुँचता है, उसके चेहरे से हर आभा ऐसे झर जाती है, जैसे वह “गोड्डा निवाणे” की किसी कठिन और थकाऊ यात्रा से लौटकर आया हो। उसे देखते हुए मन में यह शंका बार-बार जाग उठती है—कहीं ये संदेश भेजने वाले भी भीतर से वैसे ही रिक्त तो नहीं? कहीं यह मुस्कान केवल बाहरी छलावरण तो नहीं, जो भीतर के गहरे अकेलेपन को छिपाने के लिए ओढ़ रखी गई हो?
आज मेसेंजर में उमड़ती संदेशों की बाढ़ ने मेरे भीतर सामाजिक प्रवृत्तियों की तहों तक उतर जाने की एक तीव्र इच्छा जगा दी। कुछ परिचितों के जीवन-चित्र स्मृति में कौंध गए—प्रसन्न, संघर्षरत, टूटते और फिर से सँभलते हुए। हर चित्र अपने भीतर एक कहानी लिए हुए था, और हर कहानी समाज के बदलते स्वरूप का मूक प्रमाण थी।
इन सब पर विचार करते हुए सबसे पहले मैं उन परिवारों को हृदय से नमन करना चाहती हूँ जो प्रेम, धैर्य, संयम और परस्पर सम्मान की कोमल डोर से बँधे रहते हैं। ऐसे परिवार किसी नदी की गहराई जैसे होते हैं—ऊपर भले ही शांत दिखें, लेकिन भीतर वे समाज की स्थिरता और सामूहिक संतुलन के लिए अथाह जल संजोए रखते हैं। उनकी उपस्थिति समाज में शांति, सहनशीलता और स्नेही वातावरण का आधार बनती है।
किन्तु समाज का दूसरा पक्ष भी उतना ही व्यापक और तीखा है। कुछ पुरुष और स्त्रियाँ, चालीस-पैंतालीस की सीमा में पहुँचते ही अचानक “पीड़ित-भाव” की ध्वजा उठाकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपनी प्रतिभा के आकाश को छू सकते थे, यदि परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों ने उनके स्वर्णिम अवसर न निगल लिए होते। यह सोच धीरे-धीरे उनके विवाह की डोर को छिन्न-भिन्न करने लगती है। मन में उभरता यह कथित “अवसर-हरण” का भाव, दाम्पत्य जीवन में कटुता का बीज बो देता है।
इसी के समानांतर कुछ पुरुष बाहर की स्त्रियों से अपने बनावटी दर्द, झूठी विवशताओं और मनगढ़ंत दुःखों की कहानियाँ साझा करते हैं। संवेदनशील स्त्रियाँ उन कहानियों को सत्य समझकर भावनात्मक रूप से उलझ जाती हैं। पुरुषों का यह छलावा उन्हें अपने ही भावों की कैद में धकेल देता है—जहाँ वे समझ नहीं पातीं कि उनका अपनापन वास्तविकता से जुड़ा है या किसी के क्षणिक मनोरंजन का साधन मात्र।
आजकल सरायों और भोजनालयों के बाहर जो नाटकीय दृश्य घटित होते हैं—अंदर पत्नी किसी ‘मित्र’ के साथ बैठी और बाहर पति क्रोध से दहकता खड़ा—वे किसी एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की विकृत मानसकथा हैं। इन दृश्यों को देखकर लगता है कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ “विश्वास” सबसे सस्ता और “विकार” सबसे महंगा हो गया है।
कुछ लोग घर की उलझी परिस्थितियों से भागकर हमउम्र स्त्रियों या नवयुवतियों में क्षणिक सुख ढूँढने निकल पड़ते हैं। वे इन नए आकर्षणों में डूबकर यह मानने लगते हैं कि यही वास्तविक जीवन है, यही सच्चा प्रेम, यही पूर्णता। परंतु जब वह चमक भी फीकी पड़ जाती है, तो वे फिर किसी नए आकर्षण की तलाश में निकल जाते हैं—मानो जीवन कोई मण्डी हो और प्रेम उसका सबसे सस्ता सिक्का।
घर में वही व्यक्ति कलह, कड़वाहट और अव्यवस्था की आग लेकर लौटता है। मधुरता, जो वह बाहर उदारता से बाँटता है, घर की चौखट के भीतर आते ही सूख जाती है—उसकी जगह ले लेते हैं रूखे शब्द, अस्थिर मन और थकान का बोझ।
इन सब परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्त्रियों में भी प्रतिशोध, प्रतिस्पर्धा और प्रतिरोध के रूप में उभरती है। वे संघर्ष में उतर आती हैं, कभी स्वयं को सिद्ध करने, कभी अपना खोया आत्मसम्मान खोजने, तो कभी केवल अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए। इसका परिणाम होता है—परिवारों का टूटना, बच्चों में दिशाहीनता, नशे की ओर झुकाव, और कम आयु में विपरीत लिंगी आकर्षण का असामान्य उभार।
बढ़ते अपराध, एकतरफा प्रेम की त्रासदियाँ, अवसाद, आत्महत्या और हिंसा—ये सब इसी टूट चुकी पारिवारिक नींव की उपज हैं। सोशल मीडिया उन घावों पर मरहम बनने की बजाय कई बार उन्हें और गहरा कर देता है।
सुख की तलाश में लोग दूसरों की सुख-शांति भी छीन ले जाते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने घरों में संवाद, प्रेम, आदर, विश्वास और धैर्य की गरिमा को पुनः स्थापित करें। तभी हम स्वस्थ, संतुलित समाज का निर्माण कर पाएँगे—ऐसा समाज जहाँ अगली पीढ़ियाँ टूटे मनों की विरासत नहीं, बल्कि स्नेह और समझ की पूँजी लेकर आगे बढ़ सकें।
यदि मेरे शब्दों से किसी संवेदनशील हृदय को पीड़ा पहुँची हो, तो मैं सहृदय क्षमा याचना करती हूँ।
-प्रियंका सौरभ
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,