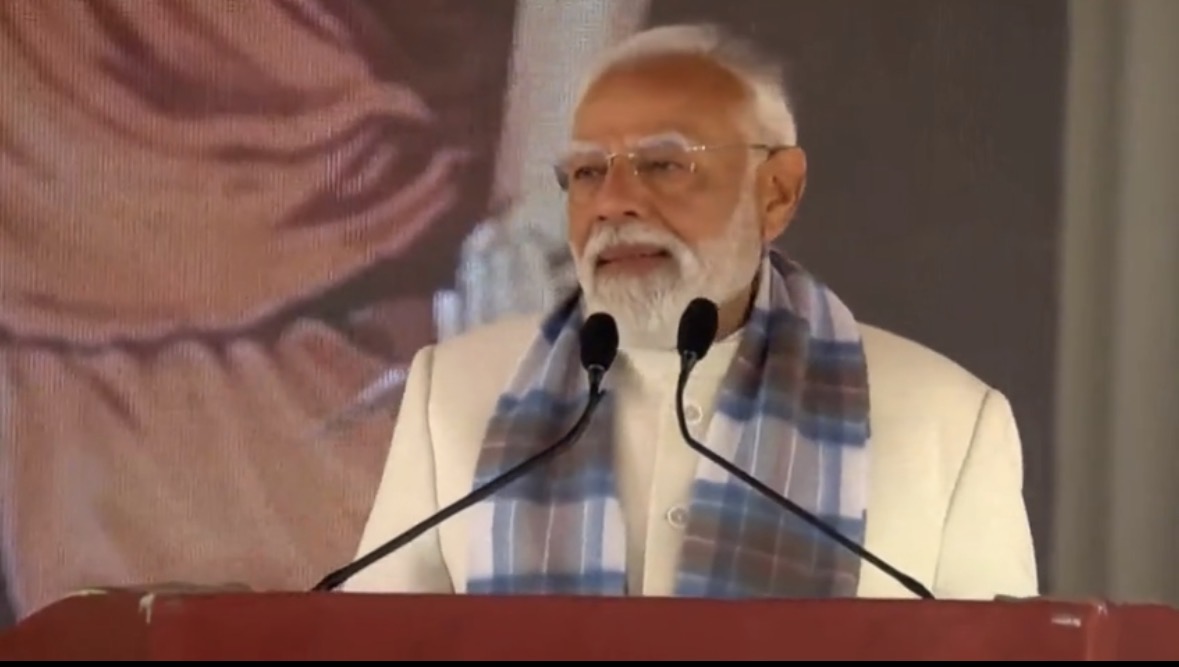तेल अवीव, 14 जनवरी (हि.स.)। इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र के छह निकायों सहित सात वैश्विक संस्थाओं पर इजराइल विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए उनसे संबंध तोड़ने की घोषणा की है।
इजराइल के विदेशमंत्री गिदोन सा’आर ने मंगलवार को यह घोषणा की। फैसले के कारणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में इजराइल विरोधी रवैया अपनाये जाने का आरोप लगाया है। सा’आर ने सात अक्टूबर को यौन हिंसा के मामलों को नजरअंदाज करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था की निंदा की और उस पर फिजूलखर्ची करने का आरोप जड़ा।
द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, विदेशमंत्री गिदोन सा’आर ने बताया कि इजराइल ने तुरंत प्रभाव से, बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के कार्यालय, लैंगिक समानता एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था यूएन वीमन, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पश्चिमी एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, सभ्यताओं का संयुक्त राष्ट्र गठबंधन, संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा तथा प्रवासन एवं विकास पर वैश्विक मंच (जीएफएमडी) को छोड़ने का फैसला किया है। जीएफएमडी संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है।
उन्होंने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि वह बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के कार्यालय के साथ सहयोग खत्म कर रहा है, क्योंकि उसने सशस्त्र संघर्ष में बच्चों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के साथ इज़राइली सेना (आईडीएफ) को भी काली सूची में डाल दिया था।
इज़राइली विदेश मंत्रालय ने अन्य छह संस्थाओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वह अन्य वैश्विक निकायों के बारे में भी विचार कर रहा है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले अमेरिका भी संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं समेत करीब 68 वैश्विक निकायों से बाहर हो चुका है।