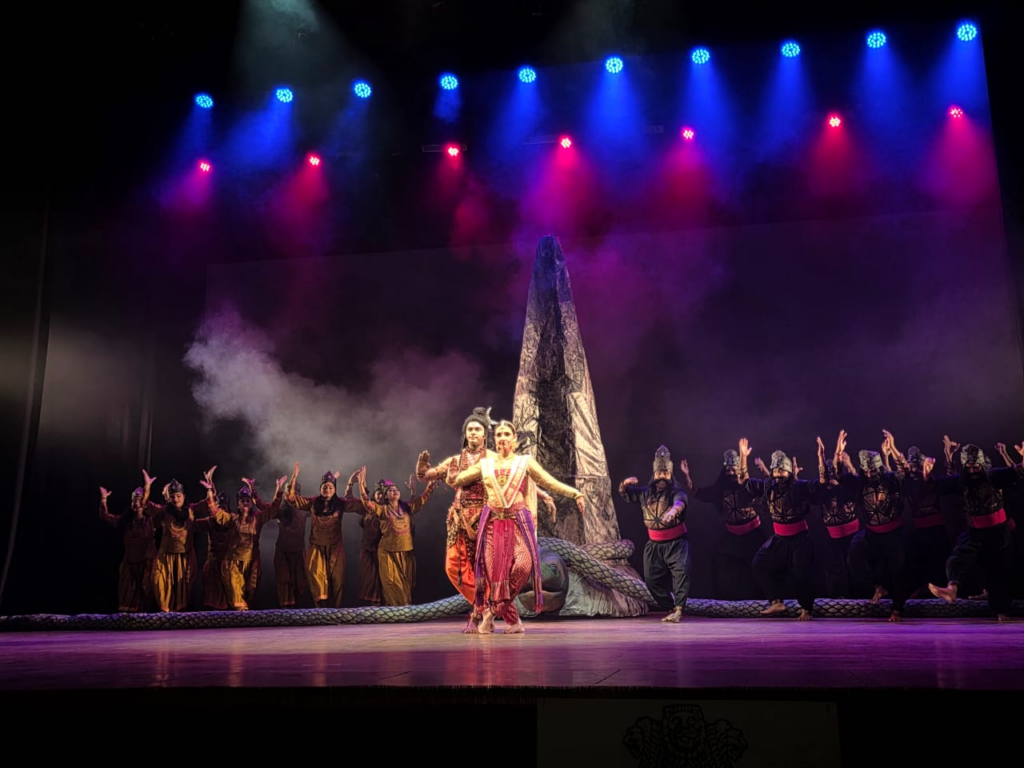– अल्मॉन्ट सिरप में भी मिला जहरीला केमिकल, जिससे छिंदवाड़ा में गई थी 25 से ज्यादा बच्चों की जान
जबलपुर/भोपाल, 13 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश में बच्चों को एलर्जी में दिए जाने वाले अल्मॉन्ट किड सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मंगलवार को राज्य सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। दरअसल, इस सिरप में भी जहरीला इंडस्ट्रियल केमिकल (खराब एथलीन ग्लायकॉल) मिला है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से गाड़ियों के कूलेंट में किया जाता है। कोल्ड्रिफ कफ सिरप में भी यही जहरीला कैमिकल मौजूद था, जिसके सेवन के बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 25 से ज्यादा मासूमों की जान चली गई थी।
मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि अल्मॉन्ट किड सिरप में जहरीला केमिकल मिलने के बाद तेलंगाना सरकार ने इसे अपने राज्य में बैन कर दिया और अन्य राज्यों को भी इसकी जानकारी भेजी है। तेलंगाना से नोटिस सभी राज्यों के पास शनिवार को आ गया था। इसके बाद इसे आगे बढ़ाते हुए हमने राज्य के हर जिले में मौजूद ड्रग इंस्पेक्टर को जानकारी भेजी है। साथ ही संबंधित सिरप को सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूरे राज्य में यह प्रक्रिया चल रही है।
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने अल्मॉन्ट किड सिरप को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए स्टाक और बिक्री पर रोक लगा दी है। जबलपुर में भी ड्रग इंस्पेक्टर ने सभी मेडिकल दुकान संचालकों को निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं पर इस सिरप को रखा है, तो उसे जमा कर दें। हालांकि ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि अभी तक जिले में स्टाक होने की जानकारी नहीं मिली है।
गौरतलब है कुछ माह पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप कांड देशभर की सुर्खियों में छाया हुआ था। यहां कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन के बाद किडनी फेल होने से 25 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। इस दौरान राज्य सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की जांच कराई थी, जिसमें केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकॉल पाए जाने की पुष्टि हुई थी। अब वही जहरीला केमिकल बच्चों को एलर्जी में दिए जाने वाले अल्मॉन्ट किड सिरप में मिला है।
तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन ने बच्चों को दी जाने वाली अल्मॉन्ट-किड सिरप पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने इस संबंध में अर्जेंट एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि इस सिरप में इथाइलीन ग्लाइकॉल नामक अत्यंत जहरीला रसायन पाया गया है। यह कार्रवाई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्राप्त लैब रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
तेलंगाना सरकार की रिपोर्ट में यह भी पुष्टि हुई है कि बिहार स्थित कंपनी ‘ट्रिडस रेमेडीज’ द्वारा निर्मित बैच नंबर एएल-24002 की यह दवा मिलावटी और जानलेवा है। यह सिरप आमतौर पर बच्चों में एलर्जी, फीवर और अस्थमा के इलाज के लिए डॉक्टरों द्वारा लिखी जाती है। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के सभी जिलों का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। दवा के विक्रय पर रोक लगाने के लिए दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, संबंधित दवा का कोई स्टॉक फिलहाल किसी के पास नहीं मिला है।
जबलपुर केमिस्ट एवं ड्रग एसोसिएशन के पूर्व सचिव चंद्रेश जैन ने बताया कि अल्मॉन्ट सिरप का बैच नंबर एएल-24002, जिसे प्रतिबंधित किया गया है, जबलपुर के किसी भी मेडिकल स्टोर या आसपास के जिलों में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि एडवाइजरी जारी की गई है कि यदि किसी दुकान पर यह सिरप मौजूद हो, तो उसे तुरंत सरेंडर कर दिया जाए। ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र जैन ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से निर्देश मिले हैं कि जिले की हर मेडिकल शॉप पर जांच की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं अल्मॉन्ट सिरप की बिक्री नहीं हो रही है। साथ ही डीलरों से भी जानकारी जुटाई जा रही है कि यदि एएल-24002 बैच का सिरप स्टॉक में हो, तो उसे तुरंत अलग कर लिया जाए।