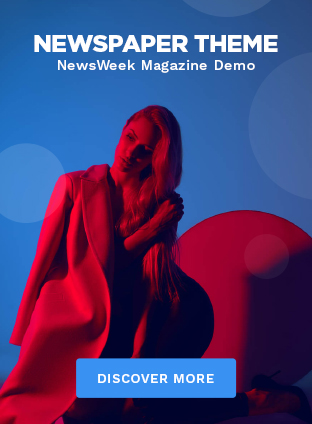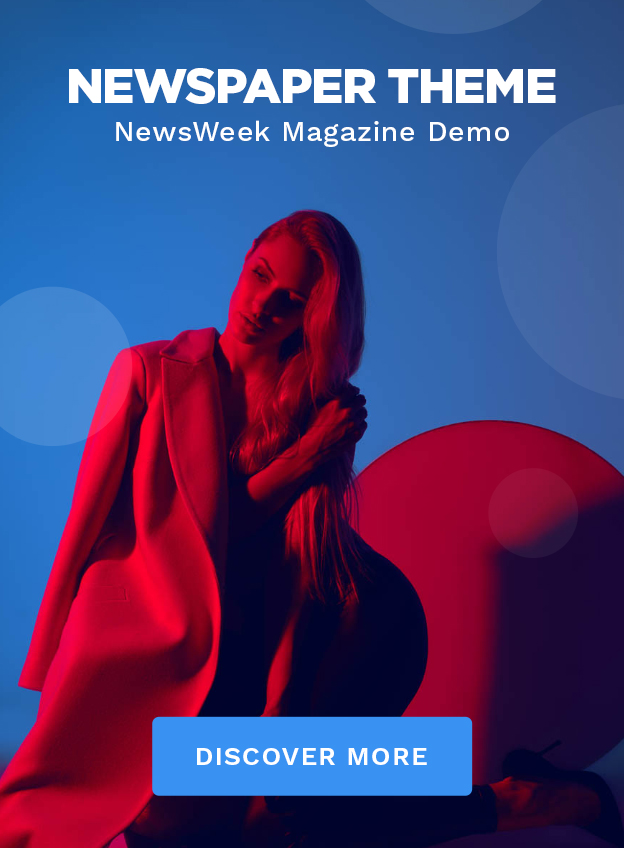हर साल 11 अक्टूबर को विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस (International Day of the Girl Child) मनाया जाता है। यह दिवस बालिकाओं के अधिकारों को पहचानने, उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह न केवल एक उत्सव का दिन है, बल्कि दुनिया भर की लड़कियों की आवाज को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक सुरक्षित, समान और समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान भी है। इस विशेष अवसर पर, भारत में बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का गहन विश्लेषण करना प्रासंगिक है।
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का महत्व और उद्देश्य
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 2011 को एक प्रस्ताव पारित करने के बाद हुई, जिसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता पर ज़ोर देना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बालिका अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सके। यह दिवस लड़कियों के शिक्षा, पोषण, चिकित्सा अधिकार, कानूनी अधिकार, और बाल विवाह जैसी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।
भारत में बालिकाओं के कल्याण और अधिकारों को समर्पित राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, जो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये दोनों दिवस मिलकर देश और विश्व स्तर पर बालिकाओं के महत्व को रेखांकित करते हैं।
भारत में बालिकाओं की स्थिति: एक जटिल तस्वीर
भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास प्राचीन काल में महिलाओं को उच्च दर्जा देने का रहा है, जहां गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। हालांकि, मध्ययुगीन काल और विदेशी शासन के दौरान समाज में अनेक कुरीतियां और विकृतियां पैदा हुईं, जिससे महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति में गिरावट आई। स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान ने लैंगिक समानता और सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों की गारंटी दी, जिसके परिणामस्वरूप बालिकाओं की स्थिति में सुधार की एक धीमी, लेकिन निश्चित यात्रा शुरू हुई।
वर्तमान में, भारत में बालिकाओं की स्थिति दो विपरीत सत्यों को दर्शाती है: एक तरफ, अभूतपूर्व प्रगति और दूसरी तरफ, गहरी जड़ें जमाए हुए सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ।
1. शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति और चुनौतियाँ
शिक्षा किसी भी बालिका के सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
सकारात्मक पहलू:
साक्षरता दर में वृद्धि: 1951 से 2011 तक स्त्री साक्षरता दर में लगभग 57.7% की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार, महिला साक्षरता दर 65.46% थी, जो 2001 में 53.67% थी।
नामांकन में सुधार: यू-डाइस रिपोर्ट (2019-20) के अनुसार, प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि सरकार के प्रयासों और सामाजिक जागरूकता के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।
उच्च शिक्षा और पेशेवर क्षेत्रों में सफलता: अब बालिकाएं केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं। वे इंजीनियरिंग, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सेना, पत्रकारिता और सॉफ्टवेयर उद्योग जैसे पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित कर रही हैं। कई बड़े शिक्षण संस्थानों में शीर्ष स्थानों पर बालिकाओं का चयन बालकों की तुलना में अधिक हो रहा है।
चुनौतियाँ:
लैंगिक साक्षरता अंतर: हालांकि साक्षरता दर बढ़ी है, फिर भी पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर मौजूद है (2011 में लगभग 16.68%)।
स्कूल छोड़ने की दर: प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक विद्यालय दूर होने या अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं।
सामाजिक कुप्रथाएं: बाल विवाह, पर्दा प्रथा और दहेज जैसी सामाजिक कुप्रथाएं आज भी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बालिका शिक्षा में बड़ी बाधा हैं।
2. स्वास्थ्य और पोषण
स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बालिकाओं को गंभीर लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है।
चुनौतियाँ:
असुरक्षित जन्म दर और कन्या भ्रूण हत्या: भारत दुनिया का इकलौता बड़ा देश है, जहां लड़कों से ज्यादा बच्चियों की मौत होती है। हालांकि, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसे अभियानों और कानूनी प्रतिबंधों के कारण जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में असमानता अभी भी बनी हुई है।
शिशु मृत्यु दर: भारत में पाँच साल से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों की तुलना में 8.3% अधिक है, जो लड़कियों के प्रति भेदभावपूर्ण पोषण और स्वास्थ्य देखभाल को दर्शाता है।
एनीमिया (रक्ताल्पता): पोषण की कमी के कारण किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है।
3. सामाजिक और कानूनी अधिकार
सामाजिक ताने-बाने में बालिकाओं के प्रति गहरी जड़ें जमाए हुए रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह हैं।
चुनौतियाँ:
भेदभाव और रूढ़िबद्धता: उन्हें अक्सर मृदुभाषी, शांत और चुप रहने की अपेक्षा की जाती है, जबकि लड़कों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है। लैंगिक भूमिकाओं से जुड़ी रूढ़िबद्धता महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव को जन्म देती है।
सुरक्षा और हिंसा: कन्या भ्रूण हत्या से लेकर यौन शोषण, हिंसा और कम उम्र में शादी तक, लड़कियों को अपने लिंग के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
बाल विवाह: 21वीं सदी में भी बाल विवाह समाज में एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जो लड़कियों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित कर देती है।
’मिसिंग विमेन’ की संख्या: 2020 में ‘मिसिंग विमेन’ (लिंग-चयनात्मक गर्भपात और स्वास्थ्य भेदभाव के कारण जन्म के समय या बाद में जीवित नहीं रहने वाली लड़कियों/महिलाओं) की अनुमानित संख्या 142.6 मिलियन थी, जो लैंगिक असमानता की भयावहता को दर्शाती है।
4. सरकारी पहल और सशक्तिकरण के प्रयास
भारत सरकार ने बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां शुरू की हैं।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP): यह योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
सुकन्या समृद्धि योजना: यह योजना बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
राष्ट्रीय बालिका दिवस: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य लड़कियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है।
स्वयं सहायता समूह (SHG): ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए स्वयं सहायता समूहों का अभियान तेजी से बढ़ रहा है।
शिक्षा के लिए प्रोत्साहन: बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण और सुरक्षित परिवहन जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
भविष्य की राह: पूर्ण सशक्तिकरण की ओर
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें याद दिलाता है कि बालिकाओं के सशक्तिकरण के बिना देश और समाज का समग्र विकास असंभव है। लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण समृद्धि और सतत विकास प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में भी शामिल है।
पूर्ण सशक्तिकरण के लिए आवश्यक कदम:
कानून का कठोर कार्यान्वयन: कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह और यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना।
शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता: प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक बालिकाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और उन्हें व्यावसायिक शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
स्वास्थ्य और पोषण में समानता: यह सुनिश्चित करना कि लड़कियों को लड़कों के समान पोषण और स्वास्थ्य देखभाल मिले, और किशोरियों के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करना।
सामाजिक सोच में बदलाव: समाज में गहरे जड़ें जमाए हुए लैंगिक पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाना। इसमें पुरुषों और लड़कों को भी समानता के समर्थक के रूप में शामिल करना महत्वपूर्ण है।
सुरक्षित वातावरण: स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर लड़कियों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना।
निष्कर्ष
भारत में बालिकाओं की स्थिति एक ऐसी कहानी है जिसमें चुनौतियों के बावजूद आशा और प्रगति की किरणें हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें उस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े होने का अवसर देता है जहां हमें केवल प्रगति का जश्न नहीं मनाना है, बल्कि बची हुई असमानताओं को दूर करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना है। जब एक बालिका सशक्त होती है, तो उसका परिवार, उसका समुदाय और अंततः उसका राष्ट्र सशक्त होता है। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, “आप किसी राष्ट्र की स्थिति को उसकी महिलाओं की स्थिति को देखकर बता सकते हैं।” भारत को एक विश्व शक्ति बनने के लिए, हर बालिका को उसकी क्षमता का एहसास करने का अवसर मिलना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हर लड़की को सिर्फ ‘बेटी’ के रूप में नहीं, बल्कि ‘देश के भविष्य’ के रूप में देखा और माना जाए।