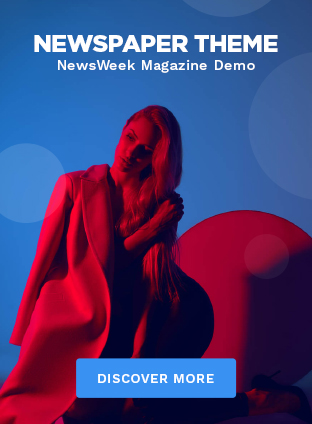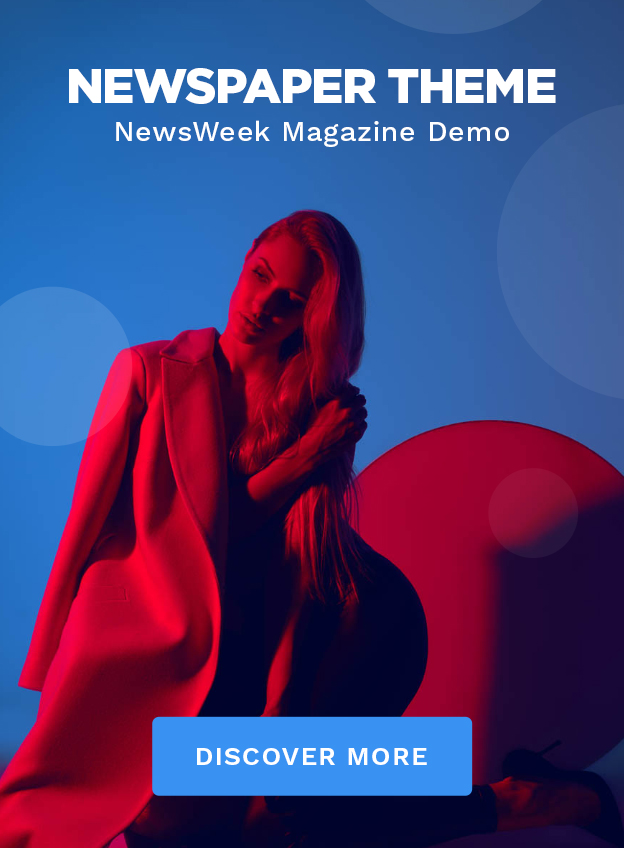विपर्यय के इन दिनों में गाँधी, जिनकी तस्वीरें आज़ादी के लगभग दो ढाई दशकों बाद तक भारतवासियों के घरों में लगभग देवपुरुषों की तरह लगी रहती थीं, अब सोशल मीडिया की दीवारों पर मीम बन कर अटपटी भदेस व्यंग्योक्तियों के साथ नज़र आते हैं। इसी के साथ यह भी नज़र आता है कि गाँधी भूमंडलीकरण के बाद के भारत में अब भी सामूहिक अंत:करण में गड़ा हुआ ऐसा काँटा हैं जिनसे निपटने के लिए उपहास, व्यंग्य, गालीगलौज सबका इस्तेमाल भी अकारथ ही सिद्ध होता है।
बहरहाल, इस पृष्ठभूमि में देखें कि हिन्दी सिनेमा में गाँधी की छाँह कैसी क्या पड़ी है।
गाँधी नाम आते ही सबसे पहले रिचर्ड एटनबरो की ‘गाँधी’ (1982) की याद आती है। गाँधी पर सबसे भव्य जीवनीपरक फ़िल्म यही है। बारह एकेडमी अवार्ड विजेता यह फ़िल्म भारत में ही नहीं दुनिया भर में सराही गई और मील का पत्थर बनी। इसने भारी कमाई भी की। बेन किंग्सले ने इसमें शीर्षक भूमिका की थी जबकि छोटी बड़ी भूमिकाओं में अनेक भारतीय कलाकार थे। प्रायः ऐसी फिल्में अपने डॉक्यु ड्रामा फॉर्मेट में निबद्ध होती हैं मगर ‘गाँधी ‘ एक सम्पूर्ण फ़ीचर फ़िल्म की तरह एक महाकाव्यात्मक चरित्र के साथ न्याय करती है। इसका जलियांवाला बाग के नरसंहार वाला दृश्य अविस्मरणीय है। बेन किंग्सले गाँधी की भूमिका में गहरे उतरे हैं और कस्तूरबा के रूप में रोहिणी हटँगड़ी बहुत जमी हैं। फ़िल्म चूँकि गाँधी के साथ साथ ही चलती है बाक़ी सभी चरित्र उनके इर्दगिर्द हाशिए पर हैं। कुछ तो सिर्फ़ दिखाई भर देते हैं।
श्याम बेनेगल की ‘ द मेकिंग ऑफ़ महात्मा ‘ (1996) गाँधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर एक अच्छी फ़िल्म है। इसमें गाँधी के महात्मा बनने से पहले का दौर है और गाँधी को एक साधारण मनुष्य की कमजोरियों के साथ चित्रित करने का उपक्रम भी। यह फ़ातिमा मीर की किताब ‘द एप्रेन्टिसशिप ऑफ़ महात्मा’ पर आधारित थी। इसका एक दृश्य स्मृति में अटक जाता है जिसमें गाँधी (रजित कपूर) अपनी पत्नी कस्तूरबा से कुछ दुर्व्यवहार करते हैं और बा (पल्लवी जोशी) उन्हें झिड़कती हैं। बेनेगल के गाँधी महान होने से पहले के ऐसे सहज मनुष्य हैं जिनकी स्वाभाविक दुर्बलताओं में किसी को भी अपना प्रतिबिंब दिखाई दे सकता है। यही इस फ़िल्म की शक्ति भी है।
2005 में एक फ़िल्म आई थी- ‘मैंने गाँधी को नहीं मारा’। इसमें अनुपम खेर ने एक ऐसे मनोरोगी की भूमिका निभाई थी जिसे गाँधी को मारने का गहरा काल्पनिक अपराध बोध है। उसकी बेटी (उर्मिला मातोंडकर) उसका ध्यान रखती है। यह व्यक्ति के रूप में एक समाज का व्यापक अपराध बोध भी हो सकता है। ‘सारांश’ के बाद अनुपम खेर अपनी इसी भूमिका को सबसे यादगार भूमिकाओं में मानते हैं। इस फ़िल्म को कम देखा गया, किंतु इसमें गहनता से एक मानवीय स्थिति को देखा गया गया है जो अपने समग्र प्रभाव में एक सामाजिक, राजनीतिक टिप्पणी भी बनती है।
अनिल कपूर ने 2007 में गाँधी और उनके बड़े बेटे हरिलाल के तनावपूर्ण सम्बन्धों पर एक फ़िल्म बनाई थी – ‘गाँधी माई फ़ादर’। इसमें हरिलाल की भूमिका में अक्षय खन्ना थे और गाँधी की भूमिका में थे दर्शन जरीवाला। यह फ़िल्म पिता पुत्र के बीच आपसी समझ के अभाव से लगा कर बेटे की बर्बादी तक की यात्रा को बहुत विचलित करने वाले ढंग से प्रस्तुत करती है। आखिर एक महान राष्ट्र का पिता कहा जाने वाला व्यक्ति अपनी सन्तान के मोर्चे पर एक असफल पिता क्यों कर साबित हुआ। एक सार्वजनिक जीवन की ये कुछ गुत्थियां अनसुलझी रह जाती हैं, जहाँ व्यक्तिगत ; सामाजिक और राजनीतिक जीवन की भेंट चढ़ जाता है। इसमें किसे दोषी माना जाए और किसे निर्दोष, यह फ़ैसला बहुत मुश्किल होता है। एक असुविधाजनक, असहज करने वाले और महात्मा को वेध्य बनाने वाले इस विषय के साथ न्याय करना आसान नहीं था और इसे किसी मर्मज्ञ और दक्ष , श्याम बेनेगल जैसे निर्देशक की आवश्यकता थी। तब भी इसे छूने के लिए निर्माता अनिल कपूर और निर्देशक फिरोज़ अब्बास खान की सराहना की जानी चाहिए। इस फ़िल्म में कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह हैं।
दर्शकों की नई पीढ़ी के लिए गाँधीवाद के बजाय गाँधीगिरी जैसा शब्द गढ़ा विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित और राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ ने। 2006 की इस फ़िल्म ने नए मुहावरे में मनोरंजन और सन्देश की मिक्स पैकेजिंग में एक तरह से गाँधी को नए दर्शकों से रूबरू करवाया। एक दृष्टिकोण से इस फ़िल्म पर गाँधी दर्शन और विचार को पनियल करने का आरोप लगाया जा सकता है मगर यह भी सही है कि इस फ़िल्म ने युवा दर्शकों में गाँधी के लिए उत्सुकता पैदा की, अहिंसक विरोध के विचार को पुनर्जीवित किया। व्यावसायिक, मनोरंजन प्रधान हिन्दी सिनेमा में गाँधी का यह अनुकूलन रेखांकित किए जाने योग्य है। मुन्ना ( संजय दत्त) और सर्किट (अरशद वारसी) के साथ बनी इस फ़िल्म में गाँधी (दिलीप प्रभवलकर) सिर्फ़ गुंडे मुन्ना भाई को दिखाई देते हैं। स्वानन्द किरकिरे ने इसके लिए गाँधी जी पर ‘बंदे में था दम’ गीत रचा जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। युवा दर्शकों के साथ कनेक्ट होती शब्दावली में, एक रंजक व्याकरण की सिनेमाई संरचना में गाँधी की यह प्रस्तुति हिन्दी सिनेमा की एक स्मरणीय रचना है। राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने इसे मेहनत और तन्मयता से लिखा और पर्दे पर साकार किया। एक संक्षिप्त अवधि में इस फ़िल्म का सामाजिक प्रभाव भी दिखाई दिया जब किसी विसंगति या अन्याय का प्रतिकार फूल देकर किया जाने लगा। यह सब भले ही लम्बा न चला हो, इसमें संदेह नहीं कि नए दर्शकों को दी गई यह गाँधीवाद की शुगरकोटेड गोली थी। यह उनका एक सहज, सरल, सुगम और सुपाच्य संस्करण अपने उन दर्शकों के लिए सुलभ कराती थी जो गाँधी से बहुत दूर चले आए हैं।
गाँधी हर युग में नए ढंग से पढ़े और प्रस्तुत किए जाएंगे। वे अपनी विभिन्न व्याख्याओं के लिए हमेशा चुनौती पेश करते हैं। उन पर तब भी ध्यान जाता है जब वे और उनके विचार समाज में अप्रासंगिक या अनुपस्थित लगने लगते हैं। फिर कोई उनकी याद करता है; फिर कोई उनकी बात छेड़ देता है। ‘सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम’ (बालक) और ‘दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के सन्त तूने कर दिया कमाल’ (जागृति ) के भावुक , गाँधी के दैवीकरण से ओतप्रोत गीतों से लगा कर ‘बंदे में था दम’ तक के गीतों और फ़िल्मों में बदलते मुहावरों में गाँधी हमारे सामने आते रहे हैं। आगे भी आते रहेंगे।
— आशुतोष दुबे