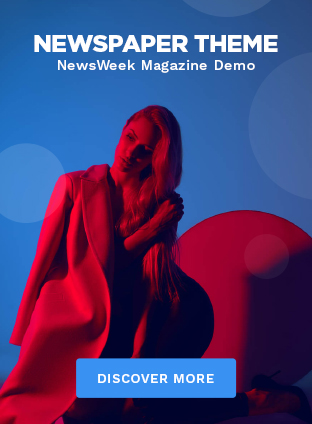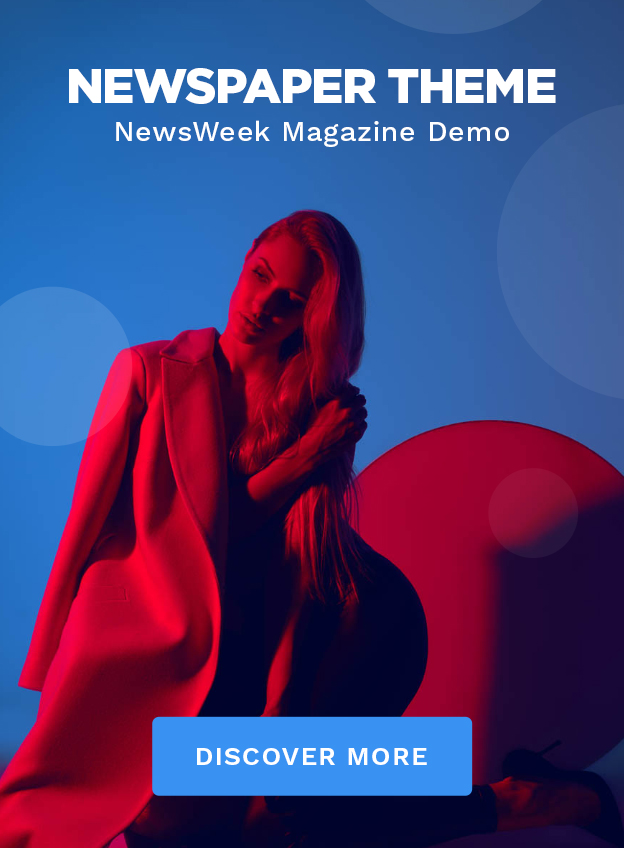लोकनायक जयप्रकाश नारायण: परिचय और भारतीय राजनीति में योगदान
जयप्रकाश नारायण (11 अक्टूबर, 1902 – 8 अक्टूबर, 1979), जिन्हें संक्षेप में जे.पी. और प्यार से ‘लोकनायक’ कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेनानी, समाजवादी विचारक और स्वतंत्रता के बाद की भारतीय राजनीति के एक महान स्तंभ थे। उनका जीवन सत्यनिष्ठा, त्याग और जनसेवा का प्रतीक था। उनका राजनीतिक सफर मार्क्सवादी रुझान से लेकर लोकतांत्रिक समाजवाद, सर्वोदय आंदोलन और अंततः ‘संपूर्ण क्रांति’ के आह्वान तक विस्तृत रहा। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया गया था।
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर, 1902 को बिहार के सिताबदियारा गाँव में हुआ था। उनके पिता हरसू दयाल एक सरकारी कर्मचारी थे और माता फूल रानी देवी थीं।इन्हें चार वर्ष तक दाँत नहीं आया, जिससे इनकी माताजी इन्हें ‘बऊल जी’ कहती थीं। इन्होंने जब बोलना आरम्भ किया तो वाणी में ओज झलकने लगा। 1920 में जयप्रकाश का विवाह ‘प्रभा’ नामक लड़की से हुआ। प्रभावती स्वभाव से अत्यन्त मृदुल थीं। गांधी जी का उनके प्रति अपार स्नेह था। प्रभा से शादी होने के समय और शादी के बाद में भी गांधी जी से उनके पिता का सम्बन्ध था, क्योंकि प्रभावती के पिता श्री ‘ब्रजकिशोर बापू’ चम्पारन में जहाँ गांधी जी ठहरे थे, प्रभा को साथ लेकर गये थे। प्रभा विभिन्न राष्ट्रीय उत्सवों और कार्यक्रमों में भाग लेती थीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में हुई। उच्च शिक्षा के लिए, वे पटना कॉलेज गए, जहाँ उन्होंने अध्ययन किया।
गांधीवादी विचारों से प्रभावित होकर, उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। बाद में, उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की, जहाँ उन्होंने बर्कले, आयोवा और विस्कॉन्सिन जैसे विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। अमेरिका में रहने के दौरान ही वे मार्क्सवाद और समाजवाद के विचारों से गहराई से परिचित हुए। 1929 में भारत लौटने पर, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए।
स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका
जयप्रकाश नारायण ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक सक्रिय और क्रांतिकारी भूमिका निभाई:
सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930): उन्होंने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जेल गए।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (1934): उन्होंने कांग्रेस के भीतर वामपंथी विचारधारा को संगठित करने के लिए आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी जैसे नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) की स्थापना की। वे इसके पहले महासचिव बने।
भारत छोड़ो आंदोलन (1942): यह उनके जीवन का सबसे क्रांतिकारी दौर था। आंदोलन के शुरुआती चरण में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वे हजारीबाग केंद्रीय कारागार से भाग निकले और भूमिगत रहते हुए स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। उनकी वीरतापूर्ण गतिविधियों ने उन्हें जनता के बीच एक “राष्ट्रीय संघर्षकर्ता” के रूप में ख्याति दिलाई।
स्वतंत्रता के बाद का योगदान
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जयप्रकाश नारायण ने सत्ता की राजनीति से परे रहकर देश की सेवा करने का मार्ग चुना और भारतीय राजनीति को कई मायनों में प्रभावित किया।
1. लोकतांत्रिक समाजवाद और दलगत राजनीति से दूरी
समाजवाद के प्रवक्ता: वे भारतीय समाजवाद के प्रमुख विचारक और प्रवक्ता रहे। उनका मानना था कि समाजवाद को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालना चाहिए।
राजनीति से संन्यास: 1950 के दशक की शुरुआत में, उन्होंने दलगत राजनीति से दूरी बना ली। उन्होंने सत्ता की राजनीति को छोड़कर जन सेवा और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि लोगों की सच्ची शक्ति नीचे के स्तर पर होनी चाहिए, न कि केवल केंद्र में।
2. सर्वोदय और भूदान आंदोलन
सर्वोदय में भागीदारी: वे महात्मा गांधी और विनोबा भावे के सर्वोदय (सबका उदय/कल्याण) दर्शन से प्रभावित हुए।
भूदान आंदोलन (1950 और 1960 के दशक): जे.पी. ने लगभग दस वर्षों तक विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन का उद्देश्य बड़े भूस्वामियों को हृदय परिवर्तन के माध्यम से अपनी भूमि गरीबों के लिए दान करने हेतु प्रेरित करना था। जे.पी. ने ग्रामदान की अवधारणा को आगे बढ़ाया, जिसमें गाँव के लोग गाँव की भूमि का सामूहिक स्वामित्व लेते थे।
3. सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान और आपातकाल
बिहार आंदोलन (1974): 1970 के दशक की शुरुआत में, देश में आर्थिक संकट, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम पर था। 1974 में, छात्रों ने बिहार में सरकारी भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। गिरते स्वास्थ्य के बावजूद, जयप्रकाश नारायण ने इस युवा नेतृत्व वाले आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग की।
सम्पूर्ण क्रांति: 5 जून, 1974 को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए, जे.पी. ने ‘सम्पूर्ण क्रांति’ का ऐतिहासिक नारा दिया। यह क्रांति किसी एक राजनीतिक परिवर्तन तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य था: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैचारिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में पूर्ण परिवर्तन लाना। उनका उद्देश्य था- भ्रष्टाचार मुक्त, समतामूलक और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना।
विपक्ष का नेतृत्व: उन्होंने इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों और कथित अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व किया और देश की जनता को एकजुट किया।
आपातकाल (1975): जब 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया, तो इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जे.पी. आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के दमन के खिलाफ लड़ने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। जेल में ही उनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया।
जनता पार्टी का गठन: आपातकाल समाप्त होने के बाद, जे.पी. ने विपक्ष के विभिन्न धड़ों को एकजुट कर जनता पार्टी का गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने 1977 के आम चुनावों में कांग्रेस को हरा कर केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई। यह भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ था।
4. लोक समाजवाद और विकेन्द्रीकरण का दर्शन
जयप्रकाश नारायण राजनीतिक शक्ति के पूर्ण विकेन्द्रीकरण में विश्वास करते थे। उन्होंने राज्य के समाजवाद के विकल्प के रूप में लोक समाजवाद को प्रस्तुत किया।
सहभागी लोकतंत्र: उनका मानना था कि शक्ति और निर्णय लेने की प्रक्रिया का आधार सबसे निचला स्तर यानी गाँव होना चाहिए। उन्होंने “सहभागी लोकतंत्र” (Participatory Democracy) की कल्पना की, जहाँ नागरिक अधिक से अधिक सक्रिय हों और सरकार के कार्यों पर कड़ी निगरानी रखें।
भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था: जे.पी. का विश्वास मूल्य की राजनीति में था। वे भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और राजनीतिक शुद्धता के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे।
विरासत और प्रभाव
जयप्रकाश नारायण ने भारतीय जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।
लोकतंत्र के रक्षक: उन्हें भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े रक्षकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने संकट के समय में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष किया।
युवा पीढ़ी का प्रेरणास्रोत: उन्होंने युवा पीढ़ी को रचनात्मक ऊर्जा और संघर्ष की भावना से प्रेरित किया और उन्हें राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए समर्पित होने का आह्वान किया।
सामाजिक न्याय के सूत्रधार: उनके विचारों और आंदोलनों ने भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय और राजनीतिक शुद्धता की माँगों को केंद्र में ला दिया।
अहिंसक क्रांति: महात्मा गांधी के बाद, जे.पी. को दूसरे ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने अहिंसक आंदोलन के माध्यम से देश की सत्ता को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर, 1979 को पटना में हुआ। उनका जीवन और कार्य हमें सिखाता है कि सच्ची राजनीति सत्ता का खेल नहीं, बल्कि जनसेवा, त्याग और नैतिक मूल्यों की स्थापना का माध्यम है। उनका ‘सम्पूर्ण क्रांति’ का आह्वान आज भी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नैतिक मार्गदर्शन का काम करता है।
।
जयप्रकाश नारायण एक निष्ठावान राष्ट्रवादी थे और सिर्फ़ खादी पहनते थे। जयप्रकाश ने रॉलेट एक्ट जलियाँवाला बाग़ नरसंहार के विरोध में ब्रिटिश शैली के स्कूलों को छोड़कर बिहार विद्यापीठ से अपनी उच्चशिक्षा पूरी की, जिसे युवा प्रतिभाशाली युवाओं को प्रेरित करने के लिए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और सुप्रसिद्ध गांधीवादी डॉ. अनुग्रह नारायण सिन्हा, जो गांधी जी के एक निकट सहयोगी रहे द्वारा स्थापित किया गया था।। जयप्रकाश जी ने एम. ए. समाजशास्त्र से किया। जयप्रकाश ने अमेरिकी विश्वविद्यालय से आठ वर्ष तक अध्ययन किया और वहाँ वह मार्क्सवादी दर्शन से गहरे प्रभावित हुए।
जयप्रकाश जी के योगदानों के बारे में जितना कहा जाए वह कम है। ये अत्यन्त परिश्रमी व्यक्ति थे। इनकी विलक्षणता की तारीफ़ स्वयं गांधीजी और नेहरू जैसे लोग किया करते थे। भारत माता को आज़ाद कराने हेतु इन्होंने तरह-तरह की परेशानियों को झेला किन्तु इन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। क्योंकि ये दृढ़निश्चयी व्यक्ति थे। संघर्ष के इसी दौर में उनकी पत्नी भी गिरफ़्तार कर ली गईं और उन्हें दो वर्ष की सज़ा हुई। क्योंकि वह भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूदी थीं और जनप्रिय नेता बन चुकी थीं। जयप्रकाश जी अपनी निष्ठा और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। वे सच्चे देशभक्त एवं ईमानदार नेता थे। वे ब्रिटिश प्रशासन का समूल नष्ट करने पर तुले हुए थे।
उन्होंने विश्व स्तर पर अपनी आवाज़ बुलन्द करते हुए कहा है कि विश्व के संकट को मद्देनज़र रखते हुए भारत को आज़ादी प्राप्त होना अति आवश्यक है। जब तक हम आज़ाद न होंगे, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व क़ायम न होगा और हम विकास के पथ पर अग्रसर न हो सकेंगे।
महात्मा गांधी ने अपने सारवान भाषण में कहा था– करो या मरो” “Do or die”
ये वाक्यांश जयप्रकाश बाबू के मन में सदैव गूँजता रहता था। फलत: उन्होंने देश को आज़ाद करने हेतु ‘करो या मरो’ का निर्णय लिया। गांधीजी के इस महामंत्र का उन्होंने जमकर प्रचार व प्रसार भी किया। गांधीजी से प्रेरणा लेकर जयप्रकाश आगे बढ़ते गये और स्वतंत्रता का बिगुल बज उठा। जब जयप्रकाश की गिरफ़्तारी हुई तो ठीक दूसरे दिन महात्मा गांधी की भी गिरफ़्तारी हुई। सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग अपने नेताओं की रिहाई की माँग करने लगे। अंग्रेज़ स्तब्ध रह गये। देश के कोने-कोने के कार्यकर्ता बन्दी बनाये गये। क्रान्ति की स्थिति सम्पूर्ण देश के सम्मुख आयी हज़ारों की संख्या में लोगों ने गिरफ़्तारियाँ दीं।
जयप्रकाश 1929 में भारत लौटने पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। भारत में ब्रिटिश हुक़ूमत के ख़िलाफ़ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण 1932 में उन्हें एक वर्ष की क़ैद हुई। रिहा होने पर जयप्रकाश ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृव्य करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी समूह था। द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में भारत की भागीदारी का विरोध करने के कारण 1939 में जयप्रकाश को दुबारा गिरफ़्तार कर लिया गया, जयप्रकाश नारायण जी को हज़ारी बाग़ जेल में क़ैद किया गया था। बापू जयप्रकाश जी के जेल से भागने की योजना बनाने लगे। इसी बीच दीपावली का त्योहार आया और जेलर साहब ने जश्न मनाने हेतु नाच-गाने का भव्य प्रोग्राम तैयार किया था, लोग मस्ती में झूम रहे थे। इसी बीच जब नाच-गाने का कार्यक्रम हुआ तो 9 नवम्बर, 1942 ई. को जयप्रकाश अपने छ: सहयोगियों के साथ धोती बांधकर जेल परिसर को लांघ गये। इसकी सूचना लन्दन तक पहुँची।
जयप्रकाश नारयण ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर 1948 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट की स्थापना की। 1953 में कृषक मज़दूर प्रजा पार्टियों के विलय में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया और चुनावी राजनीति से अलग होकर भूमि सुधार के लिए विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ गए।
जयप्रकाश जी 1974 में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक कटु आलोचक के रूप में प्रभावी ढंग से उभरे। जयप्रकाश जी की निगाह में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट व अलोकतांत्रिक होती जा रही थी। 1975 में निचली अदालत में गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने उनके इस्तीफ़े की माँग की। इसके बदले में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और नारायण तथा अन्य विपक्षी नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया। पाँच महीने बाद जयप्रकाश जी गिरफ़्तार किए गए। भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जेपी आंदोलन व्यापक हो गया और इसमें जनसंघ, समाजवादी, कांग्रेस (ओ) तथा भारतीय लोकदल जैसी कई पार्टियाँ कांग्रेस सरकार को गिराने एवं नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली के लिए एकत्र हो गईं। इस प्रकार जयप्रकाश ने ग़ैर साम्यवादी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके जनता पार्टी का निर्माण किया। जिसने भारत के 1977 के आम चुनाव में भारी सफलता प्राप्त करके आज़ादी के बाद की पहली ग़ैर कांग्रेसी सरकार बनाई। जयप्रकाश ने स्वयं राजनीतिक पद से दूर रहकर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री मनोनीत किया।
लोकनायक बाबू जयप्रकाश नारायण ने स्वार्थलोलुपता में कोई कार्य नहीं किया। वे देश के सच्चे सपूत थे और उन्होंने निष्ठा की भावना से देश की सेवा की है। देश को आज़ाद करने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। वे कर्मयोगी थे। वे अन्त: प्रेरणा के पुरुष थे। उन्होंने अनेक यूरोपीय यात्राएँ करके सर्वोदय के सिद्धान्त को सम्पूर्ण विश्व में प्रसारित किया। उन्होंने संस्कृत के निम्न श्लोक से सम्पूर्ण विश्व को प्रेरणा लेने को कहा है–
सर्वे भवन्तु सुखिन:
सर्वेसन्तु निरामया
सर्वे भद्राणी पश्यन्तु
मां कश्चिद दुखभागवेत्।।
बाबू जयप्रकाश नारायण सभी से उन्नति की बात करते थे। वे ऊँच-नीच की भेद भावना से परे थे। उनका विचार अच्छी बातों से युक्त था। वे सच्चे अर्थों में आदर्श पुरुष थे। उनके व्यक्तित्व में अदभुत ओज और तेज़ था। जयप्रकाश ने बिहार आंदोलन में भी भाग लिया है। जयप्रकाश की धर्म पत्नी श्रीमती प्रभा के 13 अगस्त सन् 1973 में मृत हो जाने के पश्चात् उनको गहरा झटका लगा। किन्तु इसके बावज़ूद भी वे देश की सेवा में लगे रहे और एक बहादुर सिपाही की तरह कार्य करते रहे। भारत का यह अमर सपूत 8 अक्टूबर सन् 1979 ई. को पटना, बिहार में चिर निन्द्रा में सो गया।
दिनकर ने लोकनायक के विषय में लिखा है–
है जयप्रकाश वह नाम
जिसे इतिहास आदर देता है।
बढ़कर जिसके पद चिह्नों की
उन पर अंकित कर देता है।
कहते हैं जो यह प्रकाश को,
नहीं मरण से जो डरता है।
ज्वाला को बुझते देख
कुंड में कूद स्वयं जो पड़ता है।।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये 1998 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरान्त भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया।