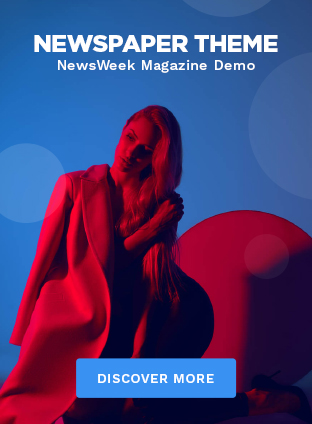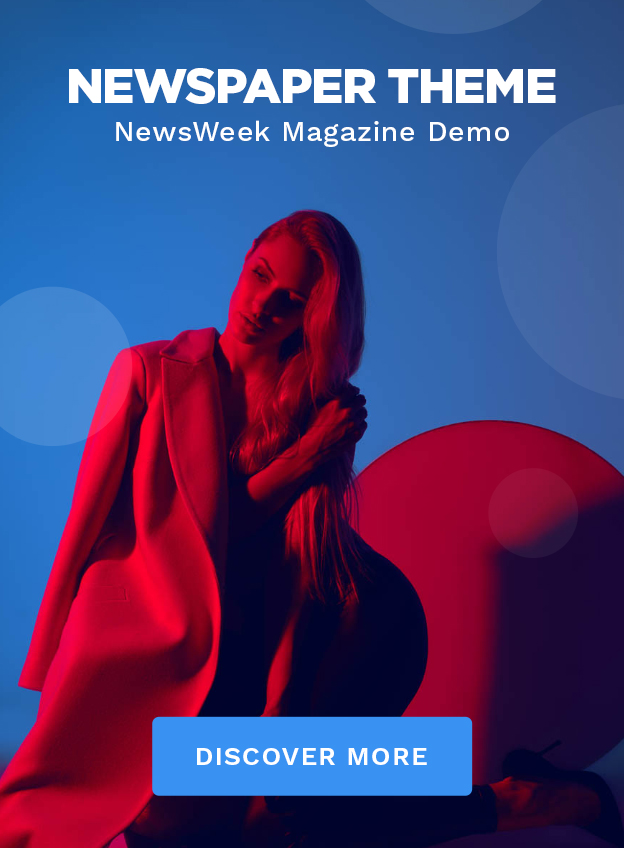भारत सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए व्यापक नीतिगत बदलावों से देश के 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों के जीवन में नई उम्मीद जगी है। चार नई श्रम संहिताओं—वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य—को लागू करते हुए केंद्र सरकार ने दावा किया है कि इससे कार्यस्थलों पर पारदर्शिता आएगी, श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा कवच मजबूत होगा, और महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल सकेगा। एक राष्ट्र—एक वेतन ढांचा, नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, ओवरटाइम का दोगुना वेतन, एक वर्ष की नौकरी पर ग्रेच्युटी, तथा संविदा और असंगठित श्रमिकों को पीएफ के दायरे में लाने जैसे बदलाव निश्चित रूप से ऐतिहासिक हैं। एक राष्ट्र—एक वेतन ढांचा, नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, ओवरटाइम का दोगुना वेतन, एक वर्ष की नौकरी पर ग्रेच्युटी, तथा संविदा और असंगठित श्रमिकों को पीएफ के दायरे में लाने जैसे बदलाव निश्चित रूप से ऐतिहासिक हैं।
यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य के अनुरूप है और श्रमिकों की दशकों पुरानी समस्याओं को हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। नया ढांचा न सिर्फ व्यवस्था को सरल करता है, बल्कि उसे अधिक मानवीय और न्यायसंगत भी बनाता है। सरकार और उद्योग—दोनों के लिए यह एक बड़ी नीतिगत उपलब्धि है।
लेकिन इस उजाले के बीच एक बड़ा वर्ग आज भी अंधेरे में खड़ा है—देश का पत्रकार समुदाय। विडंबना यह है कि जिन पत्रकारों ने श्रम सुधारों के इन दावों और उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाया, वही पत्रकार स्वयं इन सुविधाओं और अधिकारों से अक्सर वंचित हैं।
पत्रकारों की स्थिति—श्रमिकों से भी बदतर है। भारत के बड़े मीडिया घरानों में काम करने वाले पत्रकारों की आर्थिक स्थिति दिन-ब-दिन दयनीय होती जा रही है।
समस्या की जड़ें बेहद गहरी हैं: 1. नियुक्ति पत्र तक नहीं दिया जाता जबकि नए श्रम कानूनों में हर श्रमिक को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है, लेकिन बड़े मीडिया संस्थानों में हजारों पत्रकार बिना नियुक्ति पत्र के काम कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र न होने का मतलब— कोई श्रम सुरक्षा नहीं, कोई कानूनी दावा नहीं, कोई न्यूनतम वेतन सुनिश्चित नहीं।
पत्रकार खुद अपना अधिकार मांगने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि दस्तावेजी रूप से वे ‘कर्मचारी’ ही नहीं होते। वेतन संहिता पत्रकारों पर लागू नहीं होती। जिन संस्थानों से सरकार की नीतियों की खबरें निकलती हैं, वही संस्थान वेतन संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं। तय वेतन नहीं, ओवरटाइम का कोई हिसाब नहीं, समय पर भुगतान की गारंटी नहीं, पत्रकारों के लिए यह स्थिति किसी असंगठित मजदूर से कम नहीं। स्वास्थ्य सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। नए कानूनों में श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच, जोखिम क्षेत्रों में सौ प्रतिशत सुरक्षा, और स्वास्थ्य सुविधाओं की अनिवार्यता तय की गई है। लेकिन पत्रकार—जो कई बार खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं—स्वास्थ्य बीमा तक से वंचित रहते हैं।
पत्रकारों को ‘एजेंसी’ मान लेने का नया खेल। कई बड़े मीडिया हाउस अब पत्रकारों को फुल-टाइम कर्मचारी नहीं, बल्कि ‘कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी’ या ‘फ्रीलांसर’ के रूप में दर्ज कर रहे हैं। जिसका नतीजा यह होता है कि न पीएफ, न ईएसआई, न छुट्टियों का अधिकार, न ग्रेच्युटी, न नौकरी की सुरक्षा। यह व्यवस्था श्रम कानूनों से बचने का आधुनिक तरीका है।
श्रम सुधार—पत्रकारों के लिए क्यों साबित हो रहे हैं खोखले?
सरकार दावा कर रही है कि चार श्रम संहिताएँ 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करेंगी। परंतु पत्रकार, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रीढ़ हैं, सुधारों की इस श्रृंखला में शामिल ही नहीं दिखते। जब श्रमिकों को—समान वेतन, स्वास्थ्य सुरक्षा, रात्रि पाली में महिला श्रमिकों की स्वतंत्रता, भेदभाव पर रोक, ओवरटाइम का दोगुना वेतन, नौकरी के पहले साल में ही ग्रेच्युटी —जैसे अधिकार मिल रहे हैं, तब पत्रकार समुदाय आज भी बुनियादी रोजगार सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ असंगठित मजदूरों से भी कमजोर हो चुका है?
यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि:
पत्रकार बिना सुरक्षा के फील्ड में काम करते हैं। हर आर्थिक संकट में मीडिया संस्थान सबसे पहले कर्मचारियों की छंटनी करते हैं। पत्रकार यूनियनें कमजोर हो चुकी हैं। न्याय पाने के रास्ते बंद हैं, क्योंकि औपचारिक रोजगार संबंध ही स्थापित नहीं होता। ऐसे में पत्रकारों की स्थिति एक असंगठित दिहाड़ी मजदूर से भी अधिक असुरक्षित हो जाती है।
यदि सरकार का लक्ष्य वास्तव में देश के 40 करोड़ श्रमिकों में नई ऊर्जा भरना है, तो मीडिया क्षेत्र को इस दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। पत्रकार लोकतंत्र का प्रहरी हैं—और प्रहरी का कमजोर होना लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। सरकार, श्रम मंत्रालय और मीडिया नियामक संस्थानों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे:पत्रकारों के लिए विशिष्ट श्रम सुरक्षा प्रावधान। मीडिया हाउसों में नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता। पत्रकारों के लिए न्यूनतम वेतन ढांचा। स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा प्रोटोकॉल। छंटनी पर नियंत्रण और पारदर्शिता। जब तक यह न होगा, तब तक श्रम सुधार सिर्फ पोस्टर और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने रहेंगे।

नवीन चौहान , हरिद्वार