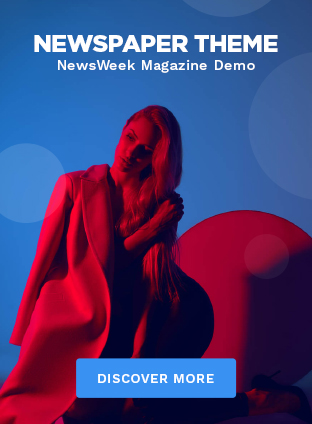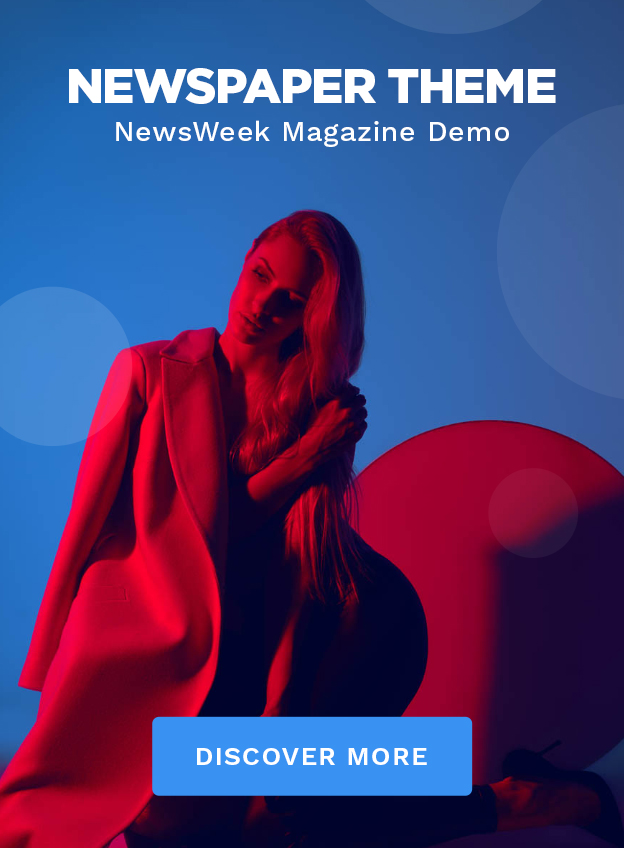लोकतंत्र में असहमति और आलोचना स्वाभाविक है। लेकिन जब विपक्ष यह कहे कि भारत भी नेपाल जैसी अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है, तो वह परोक्ष रूप से जनता को संदेश देता है कि सड़कों पर उतरकर हिंसा और तोड़फोड़ ही बदलाव का रास्ता है।
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता और वहाँ बार-बार बदलती सरकारों को आधार बनाकर भारत के विपक्षी नेता यह कह रहे हैं कि “भारत में भी ऐसे हालात हो सकते हैं।” पहली नज़र में यह बयान साधारण राजनीतिक टिप्पणी लगता है, लेकिन गहराई से देखें तो इसके गंभीर निहितार्थ हैं। यह न केवल देश की जनता को असमंजस में डालने की कोशिश है बल्कि अराजकता को हवा देने का भी प्रयास है।
लोकतंत्र में असहमति और आलोचना स्वाभाविक है। लेकिन जब विपक्ष यह कहे कि भारत भी नेपाल जैसी अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है, तो वह परोक्ष रूप से जनता को संदेश देता है कि सड़कों पर उतरकर हिंसा और तोड़फोड़ ही बदलाव का रास्ता है। इतिहास गवाह है कि जब भीड़ भड़कती है तो सबसे पहले निशाना सार्वजनिक संपत्ति बनती है— बसों को जलाना, सरकारी कार्यालयों पर हमला करना, रेलमार्ग रोकना। विपक्ष का यह बयान उसी मानसिकता को जन्म देने वाला है।
देखा जाये तो यह तुलना स्वयं में ही बेमानी है। भारत की लोकतांत्रिक जड़ें नेपाल की तुलना में कहीं अधिक मज़बूत हैं। यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, सक्रिय चुनाव आयोग है और जनता का भरोसा चुनावी प्रक्रिया में अटूट है। भारतीय मतदाताओं ने हमेशा स्पष्ट किया है कि परिवर्तन यदि होगा तो वह केवल मतदान से होगा, सड़क पर हिंसा से नहीं। ऐसे में विपक्ष का असली मक़सद यह प्रतीत होता है कि जनता में डर और असंतोष का माहौल बनाया जाए ताकि सरकार की वैधता पर सवाल खड़े हों। किंतु प्रश्न यह है कि क्या यह लोकतांत्रिक राजनीति है या केवल अवसरवादी रणनीति? लोकतंत्र में असहमति संविधान की मर्यादाओं में रहकर व्यक्त की जानी चाहिए, न कि अराजकता का वातावरण बनाकर।
विपक्षी नेताओं को यह समझना होगा कि नेपाल और भारत की परिस्थितियों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। भारत में संस्थाएँ सुदृढ़ हैं और जनता का विश्वास स्थिरता व विकास में है। नेपाल का हवाला देकर भारत को अस्थिर बताना केवल जनता को भड़काने का प्रयास है, जिसका अंतिम परिणाम राष्ट्रहित के विरुद्ध ही होगा। लोकतंत्र की असली ताक़त जनता का विश्वास और संवैधानिक प्रक्रिया में आस्था है। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि भारत में परिवर्तन की राह हिंसा या अराजकता से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक माध्यमों से ही निकलेगी।
इसके अलावा, “नेपाल जैसा आंदोलन” भारत में दोहराया जा सकता है या नहीं, इसका विश्लेषण कुछ बिंदुओं में करना ज़रूरी है। सबसे पहले नेपाल के संदर्भ को देखें तो वहां 2006 का जनआंदोलन (लोकतांत्रिक आंदोलन) राजशाही को समाप्त करके गणतंत्र लाने का कारण बना। उसके पीछे कुछ खास परिस्थितियाँ थीं। जैसे- लंबे समय से चली आ रही राजशाही और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का टकराव देखने को मिल रहा था। माओवादी विद्रोह और सशस्त्र संघर्ष से दबाव उपजा हुआ था। राजनीतिक दलों और जनता का राजशाही के खिलाफ़ व्यापक एकजुट होना भी एक कारण था।
वहीं भारत की परिस्थितियाँ नेपाल से बिल्कुल अलग हैं। भारत 1947 से ही एक लोकतांत्रिक गणराज्य है; यहाँ राजशाही जैसी व्यवस्था का अवशेष नहीं है। भारत का संविधान अत्यंत मज़बूत है और इसमें लोकतांत्रिक अधिकारों, संघीय ढांचे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्पष्ट सुरक्षा प्राप्त है। साथ ही भारत का राजनीतिक परिदृश्य बहुदलीय है, यहां विभिन्न विचारधाराओं को मंच मिलता है, जिससे असंतोष विद्रोह में बदलने से पहले ही संस्थागत रास्ता खोज लेता है। इसके अलावा, भारतीय सेना और सुरक्षा तंत्र राजनीतिक रूप से तटस्थ हैं, जबकि नेपाल में राजशाही का सीधा प्रभाव सेना पर था।
देखा जाये तो संवैधानिक संकट या राजशाही विरोध जैसा आंदोलन भारत में संभव नहीं है क्योंकि यहाँ राजशाही या निरंकुश शासन की गुंजाइश ही नहीं है। जनता के बड़े आंदोलन (जैसे 1975-77 का आपातकाल विरोध, 2011 का अन्ना हज़ारे आंदोलन, किसान आंदोलन आदि) भारत में हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं। लेकिन ये आंदोलन संवैधानिक ढांचे के भीतर रहते हैं और सत्ता-परिवर्तन लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानि चुनाव से ही होता है। भारत की विविधता, लोकतांत्रिक संस्थाएँ और संघीय ढांचा किसी एक समूह या विचारधारा को पूरे देश पर “क्रांतिकारी” ढंग से हावी होने नहीं देता।
देखा जाये तो भारत का लोकतंत्र दुनिया के सबसे जीवंत और विविध लोकतंत्रों में से एक है। यहाँ असहमति और विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक परंपरा का स्वाभाविक हिस्सा रहे हैं। पिछले पाँच दशकों में कई ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने देश की राजनीति की दिशा बदल दी, लेकिन महत्वपूर्ण यह रहा कि ये बदलाव लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर ही संपन्न हुए। यही वह अंतर है जो भारत को पड़ोसी देशों की उथल-पुथल से अलग करता है।
1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताएँ सीमित कर दी गईं। प्रेस सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और राजनीतिक दमन ने जनता में गुस्सा भर दिया। दो साल बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने इंदिरा गांधी की सरकार को सिरे से नकार दिया। आपातकाल का विरोध साबित करता है कि भारत में जनता अंततः लोकतंत्र की बहाली और सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम है।
इसके अलावा, भ्रष्टाचार के खिलाफ़ अन्ना हज़ारे का जनांदोलन युवाओं और शहरी मध्यम वर्ग का प्रतीक बन गया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे और जनलोकपाल की मांग गूँजने लगी। इस आंदोलन ने दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार को सत्ता से हटा दिया और केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ भी नाराजगी पैदा की। इसके परिणामस्वरूप आम आदमी पार्टी जैसी नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। इस तरह से सत्ता में बदलाव लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के ज़रिए हुआ।
वहीं तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का लंबे समय तक चला आंदोलन भी भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का उदाहरण है। लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे, लेकिन आंदोलन लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर ही चला। अंततः सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। यह घटना बताती है कि भारत में जनता शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से सरकार की नीतियों को बदलने की ताक़त रखती है।
इन तीनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि भारत में आंदोलन सत्ता को हिला सकते हैं, सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन यह सब संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा के भीतर होता है। न तो नेपाल जैसी राजशाही उखाड़ने की स्थिति बनी, न ही सैन्य हस्तक्षेप की। भारत की जनता लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था रखती है और यही भारत के राजनीतिक ताने-बाने की सबसे बड़ी शक्ति है। लोकतंत्र की यही खूबी है कि यहाँ असहमति बग़ावत नहीं बनती, बल्कि बदलाव का वैधानिक मार्ग प्रशस्त करती है।
इसके अलावा, 2014 से अब तक भारत ने राजनीतिक स्थिरता का जो अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह दुनिया के कई बड़े लोकतांत्रिक देशों और पड़ोसी राष्ट्रों की स्थिति से बिल्कुल अलग खड़ा होता है। दुनिया के सबसे अमीर देशों के समूह जी-7 पर नज़र डालें तो पिछले दस वर्षों में वहां नेतृत्व बदलने की परंपरा लगातार जारी रही है। अमेरिका में बराक ओबामा से लेकर ट्रम्प और बाइडेन और फिर ट्रम्प तक नेतृत्व बदला। ब्रिटेन में डेविड कैमरन से रिषि सुनक और अब कीर स्टारमर तक प्रधानमंत्री बदलते गए। इटली और जापान में भी प्रधानमंत्री बार-बार बदले। जर्मनी, कनाडा और फ्रांस में भी नेतृत्व का स्वरूप बदला। इन बड़े लोकतंत्रों में अस्थिरता सामान्य बात रही।
भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति और भी नाटकीय रही। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कुर्सी का बार-बार बदलना अब चलन-सा हो गया है। नवाज़ शरीफ, इमरान ख़ान और शहबाज़ शरीफ सभी इस दौर में आ-जा चुके हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट ने सरकारें हिला दीं, नेपाल में गठबंधन की राजनीति ने स्थिरता को ग्रहण लगा दिया और बांग्लादेश में भी राजनीतिक टकराव ने नेतृत्व को अस्थिर किया।
इन सबके बीच भारत ने 2014 से एक ही नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए स्थिरता की मिसाल कायम की है। जनता ने लगातार तीन बार उन्हें सत्ता सौंपी। मोदी की लगातार जीत केवल चुनावी रणनीति की सफलता नहीं, बल्कि उस विश्वास का प्रमाण है जो जनता उनके नेतृत्व में महसूस करती है। मोदी की राजनीति का मूल मंत्र है— जनता से सीधा संवाद, विकास की ठोस योजनाएँ और राष्ट्रहित में निर्णायक फैसले। स्वच्छ भारत से लेकर डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत तक, उनकी हर पहल ने जनता को जोड़ा है और भरोसा जगाया है। मोदी की कार्यशैली कर्मठ, दृढ़ और दूरदर्शी मानी जाती है। आलोचना के बावजूद उनकी छवि उस नेता की है जो सिर्फ़ बोलता नहीं, बल्कि काम करके दिखाता है।
बहरहाल, देखा जाये तो आज जब विश्व की बड़ी ताक़तें नेतृत्व की अस्थिरता से जूझ रही हैं, भारत का लोकतंत्र नरेंद्र मोदी के रूप में निरंतरता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यही वह राजनीतिक पूँजी है जिसने भारत को न केवल अपने भीतर स्थिर रखा है, बल्कि दुनिया में भी एक आत्मविश्वासी और सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा किया है। यह सब मिलकर दिखाता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा नेतृत्व हैं जिसे जनता ने “विश्वास के साथी” के रूप में स्वीकार किया है और यही कारण है कि 2014 से भारत में शासन उनके हाथों में बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। इसलिए विपक्ष के जो लोग भारत में नेपाल जैसे घटनाक्रम का सपना देख रहे हैं उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहने दीजिये। ऐसे सपने देखने वाले नेता ना तो जनता पर विश्वास करते हैं ना ही खुद पर इसलिए वह आपदा में अवसर की तलाश में हैं।
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)