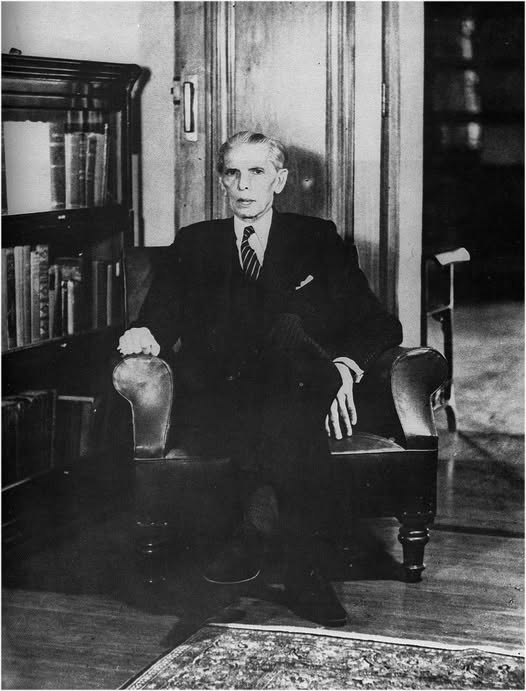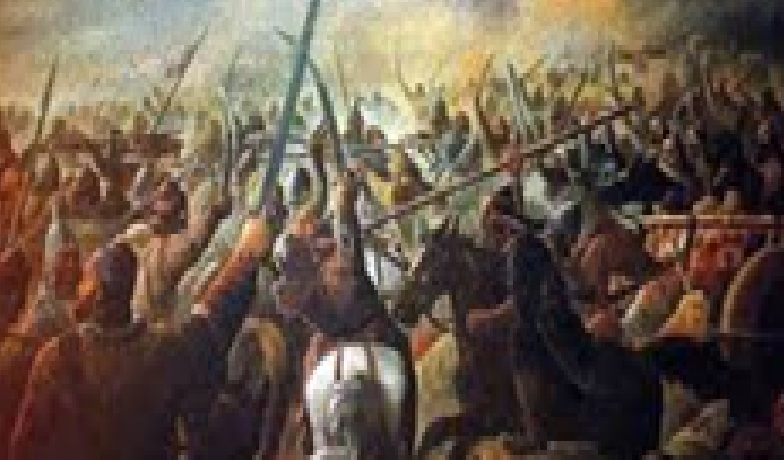16 तक लगा सकेंगे बोली

नई दिल्ली, 13 जनवरी (हि.स.)। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी इंडो एसएमसी का 91.95 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 16 जनवरी तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 19 जनवरी को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 20 जनवरी को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 21 जनवरी को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं।
इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 141 रुपये से लेकर 149 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1,000 शेयर का है। इंडो एसएमसी के इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स दो को लॉट यानी 2,000 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 2,98,000 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 61.71 लाख नए शेयर जारी हो रहे हैं।
आईपीओ खुलने से एक कारोबारी दिन पहले 12 जनवरी को इंडो एसएमसी ने 11 एंकर इनवेस्टर्स से 26.16 करोड़ रुपये जुटाए। इन एंकर इनवेस्टर्स में बंगाल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड सबसे बड़ा इनवेस्टर रहा। इसने कंपनी से अपर प्राइस लिमिट 149 रुपये प्रति शेयर की दर से 3.05 लाख शेयर खरीदे हैं। इसी तरह 360 वन एलवीएफ ट्रेजरी सॉल्यूशंस फंड कंपनी से 1.18 लाख शेयर खरीद कर दूसरा सबसे बड़ा एंकर इनवेस्टर बना है।
इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 47.45 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 33.25 प्रतिशत हिस्सा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 14.29 प्रतिशत हिस्सा और मार्केट मेकर्स के लिए 5.01 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इस इश्यू के लिए जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स प्रा.लि. को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। वहीं गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग प्रा.लि. और निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड कंपनी के मार्केट मेकर हैं।
कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत में लगातार मजबूती आई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 46 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर तीन करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी का शुद्ध लाभ उछल कर 15.44 करोड़ रुपये रह गया। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2025 में कंपनी को 11.46 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हो चुका है।
इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी लगातार बढ़ोतरी होती रही। वित्त वर्ष 2022-23 में इसे 7.30 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 28.06 करोड़ और वित्त वर्ष 2024-25 में उछल कर 138.78 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2025 में कंपनी को 112.62 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है।
इस अवधि में कंपनी के कर्ज में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में कंपनी पर 10.43 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 17.70 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में उछल कर 35.76 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही के अंत यानी 30 सितंबर तक कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ 49.35 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।
इस अवधि में कंपनी के रिजर्व और सरप्लस में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2022-23 में ये 52 लाख रुपये के स्तर पर था, जो 2023-24 में बढ़ कर 5.06 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह 2024-25 में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस 19 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2025 तक ये 30.46 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
इसी तरह ईबीआईटीडीए (अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट, टैक्सेज, डिप्रेशिएशंस एंड एमॉर्टाइजेशन) 2022-23 में 1.15 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2023-24 में बढ़ कर 5.08 करोड़ रुपये हो गया। साल 2024-25 में कंपनी का ईबीआईटीडीए उछल कर 22.83 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही के अंत यानी सितंबर 2025 तक ये 17.19 करोड़ रुपये के स्तर पर था।