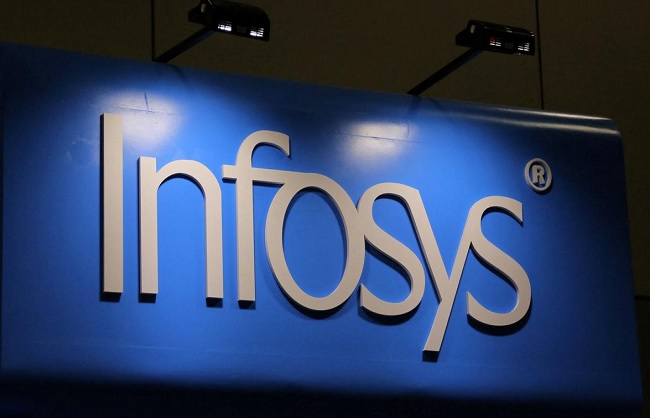निर्मल रानी
प्रसिद्ध हिंदी लेखक, पत्रकार और पटकथा लेखक कमलेश्वर ने सम्मान,एवार्ड अथवा पुरस्कार के विषय पर बातचीत करते हुये एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी ‘सम्मान’ ग्रहण करने से पहले यह ज़रूर देखना चाहिये कि सम्मानित करने वाली संस्था या व्यक्ति का स्वयं अपना कितना ‘सम्मान’ है। ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा था कि तमाम लोग व संस्थाएं विशिष्ट लोगों को सम्मानित करने के नाम पर या इसी के बहाने ख़ुद अपनी छवि चमकाने या स्वयं की प्रसिद्धि की ख़ातिर तरह तरह के सम्मान समारोह आयोजित करती रहती हैं। ऐसे में सम्मान या पुरस्कार प्राप्त करने के लिये लालायित रहने वाले लोग तो किसी भी ऐरे ग़ैरे नत्थू ख़ैरे से कोई भी सम्मान लेने पहुँच जाते हैं। यहाँ तक कि सम्मान हासिल करने के लिये तरह तरह की जुगाड़बाज़ियाँ भी करते हैं। परन्तु स्वाभिमानी लोग या ऐसे सम्मान की वास्तविकता को समझने वाले लोग इसतरह के कथित पुरस्कारों व सम्मानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं ।
कुछ ऐसा ही दृश्य पिछले दिनों उस समय देखने को मिला जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कांग्रेस नेता शशि थरूर को ‘सावरकर’ के नाम का एक अवार्ड देने की कोशिश की गयी परन्तु शशि थरूर ने इसे लेने से इंकार कर दिया। ग़ौर तलब है कि केरल की ‘हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ‘(HRDS इंडिया) नाम के एक एनजीओ ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को ‘वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2025’ का पहला अवार्ड देने की कोशिश की थी। HRDS इंडिया को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस ) या संघ परिवार से संबद्ध माना जाता है। बात बीते वर्ष दिसंबर माह की है, जब केरल-आधारित इस एनजीओ ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को ‘वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2025’ का पहला प्राप्तकर्ता घोषित किया। HRDS इंडिया के अनुसार यह पुरस्कार राष्ट्रीय विकास, सामाजिक सुधार और मानवीय कार्यों के लिए दिया जाता है, और इसका नाम विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) के नाम पर रखा गया है, जो भाजपा और संघ परिवार द्वारा सम्मानित व आदर्श पुरुष माने जाते हैं। जबकि कांग्रेस,उदारवादियों और वामपंथी दलों द्वारा उनकी स्वतंत्रता संग्राम में कथित नकारात्मक भूमिका पर सवाल उठाए जाते हैं। यह पुरस्कार सम्मान समारोह 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में आयोजित होना प्रस्तावित था। इस आयोजन का उद्घाटन भी भाजपा के वरिष्ठ नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जाना था। संस्था द्वारा इस पुरस्कार हेतु थरूर का नाम उनके राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हस्तक्षेप और प्रभाव के लिए चुना गया था। परन्तु थरूर ने इस पुरस्कार को स्वीकार करने से यह कहते हुये इंकार कर दिया कि उन्हें इस पुरस्कार की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली थी न कि आयोजकों से।
ग़ौरतलब है कि शशि थरूर इस समय तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद हैं। उन्होंने मीडिया से पूछने पर स्वयं यह स्पष्ट किया कि था कि वे इस पुरस्कार के बारे में नहीं जानते थे और न ही इसे स्वीकार करने की सहमति जताई थी । सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके भी उन्होंने यही कहा कि “मैं न तो इस पुरस्कार के बारे में जानता था और न ही इसे स्वीकार किया था। आयोजकों द्वारा मेरी सहमति के बिना मेरे नाम की घोषणा करना ग़ैर -ज़िम्मेदाराना है। पुरस्कार की प्रकृति, प्रस्तुत करने वाली संस्था या अन्य संदर्भों के बारे में स्पष्टता न होने पर, मैं न तो कार्यक्रम में भाग लूंगा और न ही पुरस्कार स्वीकार करूंगा”। थरूर ने सावरकर के व्यक्तित्व पर सीधे टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनका इनकार कांग्रेस की वैचारिक स्थिति से जुड़ा माना जा रहा है। कांग्रेस में उनके सहयोगियों का मानना था कि सावरकर के नाम पर पुरस्कार स्वीकार करना पार्टी का अपमान होगा व ऐसा करना पार्टी को शर्मिंदा करेगा। थरूर पहले सावरकर पर किताब लिख चुके हैं और उनका कहना है कि सावरकर का अध्ययन ज़रूरी है, लेकिन आलोचनात्मक रूप से।
उधर HRDS इंडिया के आयोजकों ने इस विषय पर यह दावा किया था कि थरूर को इस पुरस्कार के बारे में पहले से जानकारी दी गई थी और उन्होंने अपनी सहमति भी जताई थी। परन्तु थरूर ने संस्था के इस दावे को पूरी तरह ख़ारिज कर दिया। आख़िरकार यह विवाद इतना बढ़ा कि विवाद के बाद न तो सम्मान प्राप्तकर्ता के रूप में शशि थरूर ने कार्यक्रम में शिरकत की ना ही सम्मान देने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में पधारे। परन्तु इस घटना के बाद सावरकर के नाम को लेकर एक बार फिर उनके विवादित व्यक्तित्व को लेकर बहस ज़रूर छिड़ गयी। ग़ौरतलब है कि संघ व भाजपा सावरकर को ‘वीर सावरकर ‘ कहकर बुलाती है और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्हें सम्मान देती है। जबकि कांग्रेस उन्हें ब्रिटिश हुकूमत से मुआफ़ी मांगने वाला व्यक्ति मानती है। निश्चित रूप से शशि थरूर का सावरकर सम्मान लेने से इंकार करना न केवल कांग्रेस में उनकी स्थिति को मजबूत करता है बल्कि वैचारिक रूप से सावरकर की हिंदूवादी राजनीति को भी ख़ारिज करता है।
इस घटना ने संघ व भाजपा परिवार की उस ‘चतुराई ‘ को भी एक बार फिर उजागर कर दिया है जिसके तहत वह कांग्रेस अथवा अन्य धर्मनिरपेक्ष व उदारवादी नेताओं को किसी न किसी बहाने अपने साथ खड़ा हुआ दिखाने की कोशिश करती रहती है। साथ ही ऐसा कर उन्हें कांग्रेस में भी वैचारिक रूप से असहज करने का प्रयास करती है। हालांकि संघ व भाजपा की इस नीति से यह सन्देश भी जाता है कि उनके पास इस स्तर के अपनी विचारधारा रखने वाले नेताओं की भी कमी है। चाहे वह महात्मा गाँधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाने वाले कांग्रेस नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा बनाना हो या फिर जून 2018 में कांग्रेस नेता व पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को संघ के तृतीय वर्ष शिक्षा वर्ग समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नागपुर में आमंत्रित करना।
इसी सिलसिले की एक कड़ी के रूप में शशि थरूर को सावरकर सम्मान के नाम पर दिया गया कथित निमंत्रण भी उन्हें कांग्रेस में असहज करने व वैचारिक रूप से उन्हें अपने पक्ष में खड़ा दिखाने का प्रयास था परन्तु यह प्रयास तब उल्टा पड़ गया जब शशि थरूर ने स्वयं इस ‘गले पड़े’ पुरस्कार को लेने से इंकार कर उल्टे इस पुरस्कार का ही ‘तिरस्कार ‘कर दिया।
निर्मल रानी