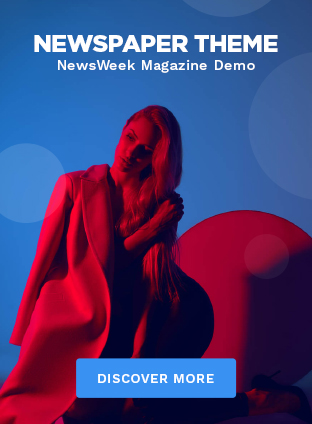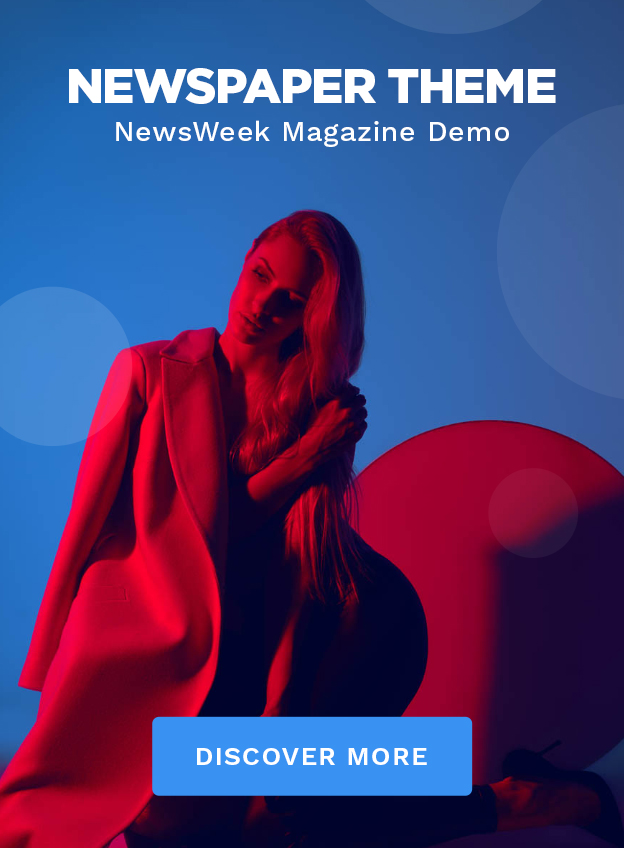तवायफ की बेटी से सुरों की रानी तक का संघर्ष
मल्लिका-ए-ग़ज़ल: बेगम अख़्तर की मां मुश्तरी बाई एक तवायफ थीं, और समाज ने इस पहचान के साथ हमेशा भेदभाव किया। लोग अख्तरी बाई की गायकी से तो प्रभावित हुए, पर उन्हें सिर्फ एक “कोठे की गायिका” कहकर सीमित कर दिया। एक बार एक तवायफ संगठन ने मुश्तरी बाई से कहा कि वह अपनी बेटी को एक लाख रुपये में सौंप दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी को कोठे से निकालकर मंच तक पहुंचाया। और वही अख्तरी बाई, बाद में बेगम अख्तर बनीं—वो नाम जिसने ग़ज़लों को कोठों से निकालकर घर-घर में पहुंचाया।
बेगम अख्तर की ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय था उनका शोषण। 13 साल की उम्र में बिहार के एक राजा ने उन्हें गायन के बहाने बुलाया और उनके साथ बलात्कार किया। इससे वह गर्भवती हुईं और एक बेटी ‘शमीमा’ को जन्म दिया। समाज के डर से वह अपनी बेटी को “छोटी बहन” बताती रहीं। यह रहस्य कई सालों बाद खुला। इस त्रासदी ने उनके सुरों में जो दर्द भरा, वही उनकी ग़ज़लों की रूह बन गया। शायद यही कारण था कि उनकी आवाज़ में दर्द इतना सजीव लगता था।
ग़ज़लों की मल्लिका – जब सुरों ने पाई पहचान
1940 के दशक में बेगम अख्तर ने एचएमवी कंपनी के साथ करार किया और कई ग़ज़लें, ठुमरी और दादरे रिकॉर्ड किए। उन्होंने ग़ालिब, फैज़ अहमद फैज़, कैफ़ी आज़मी, शकील बदायूनी जैसे बड़े शायरों के कलाम गाकर उन्हें अमर कर दिया। उनके सुरों ने ग़ज़लों को कोठों की दीवारों से निकालकर सभ्य समाज तक पहुंचाया। तभी उन्हें “मल्लिका-ए-ग़ज़ल” कहा जाने लगा। मशहूर शायर कैफ़ी आज़मी ने कहा था—“ग़ज़ल के दो मायने हैं—एक ग़ज़ल और दूसरा बेगम अख्तर।”
सिगरेट के लिए रुकी ट्रेन – बेगम का अंदाज़-ए-जिंदगी
बेगम अख्तर की आदतें भी उतनी ही अलग थीं जितनी उनकी गायकी। वह अकेलेपन से डरती थीं, इसलिए सिगरेट और शराब का सहारा लिया। एक बार ट्रेन में सफर के दौरान उन्हें सिगरेट नहीं मिली तो उन्होंने ट्रेन ही रुकवा दी। गार्ड की लालटेन और झंडा लेकर बोलीं—“जब तक सिगरेट नहीं आती, ट्रेन नहीं चलेगी।” ऐसी थी उनकी बेबाकी। उनकी लत इतनी गहरी थी कि फिल्म पाकीज़ा उन्होंने छह बार में पूरी देखी, क्योंकि हर बार सिगरेट पीने बाहर चली जाती थीं।
शादी, विराम और फिर सुरों की वापसी
1945 में उन्होंने लखनऊ के बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी की और यहीं से बनीं “बेगम अख्तर।” पति के कहने पर उन्होंने गाना छोड़ दिया, लेकिन संगीत के बिना वह बीमार रहने लगीं। 1949 में उन्होंने फिर मंच पर वापसी की और तीन ग़ज़लें व एक दादरा गाया। इसके बाद उन्होंने कभी माइक नहीं छोड़ा। उनके लिए संगीत सिर्फ कला नहीं, जीवन का प्राण था।
आखिरी सांस तक गाती रहीं बेगम अख्तर
7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद की एक साधारण सी बच्ची ‘अख्तरी बाई’ ने जन्म लिया। कोई नहीं जानता था कि यही बच्ची आगे चलकर “मल्लिका-ए-ग़ज़ल” कहलाएगी। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था जो दिलों को छू जाता था। लेकिन इस मधुर आवाज़ के पीछे कितनी कड़वी सच्चाइयाँ थीं, यह बहुत कम लोग जानते हैं। पिता असगर हुसैन, जो पेशे से वकील थे, ने माँ मुश्तरी बाई और दोनों बेटियों को छोड़ दिया। एक जुड़वा बहन बचपन में ज़हरीली मिठाई से चल बसी। बचपन से ही बिब्बी यानी अख्तरी बाई का जीवन दर्द से शुरू हुआ, जो उनके सुरों में घुलकर अमर हो गया।
पहली ताल – जब सुर बने ज़िंदगी की पहचान
अख्तरी बाई को बचपन से संगीत की ललक थी। उस्ताद मोहम्मद खान से उन्होंने रियाज़ शुरू किया। शुरुआत में जब सुर नहीं लगते थे, उस्ताद ने डांट दी, और नन्ही बिब्बी
ने कहा—”अब मैं नहीं सीखूंगी।” लेकिन उस्ताद के प्यार ने उन्हें वापस सुरों की ओर खींच लिया। यही मोड़ था जहां से संगीत उनकी ज़िंदगी बन गया। 15 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार स्टेज पर गाया। सरोजिनी नायडू जैसी हस्ती उनकी आवाज़ पर मंत्रमुग्ध हो गईं और उन्हें साड़ी भेंट की। तभी लोगों ने जाना—एक नई आवाज़ का जन्म हुआ है।
1974 में अहमदाबाद के एक मंच पर वह कैफ़ी आज़मी की ग़ज़ल गा रही थीं। तबीयत बेहद खराब थी, लेकिन उन्होंने गाना बंद नहीं किया। दर्शक तालियों से गूंज उठे, और वह मुस्कुराते हुए मंच से नीचे उतरीं। उसी दिन, 30 अक्टूबर 1974 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वह आखिरी वक्त तक गाती रहीं। लखनऊ के पसंदा बाग में आज भी उनकी मजार पर लोग ग़ज़लों की महक महसूस करते हैं।
पाकिस्तान में भी बजता रहा सुरों का जादू
1959 में बेगम अख्तर लाहौर गईं और पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गाईं। 1970 में उन्होंने कराची रेडियो के लिए कई ग़ज़लें और ठुमरियां रिकॉर्ड कीं। वहां भी उनकी आवाज़ को उतना ही सम्मान मिला जितना हिंदुस्तान में। ग़ज़ल को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में उनका योगदान अद्वितीय है।
अमर हो गया दर्द, सुर और आत्मा
बेगम अख्तर सिर्फ गायिका नहीं थीं, वो भावनाओं की आवाज़ थीं। उनके हर सुर में एक कहानी थी, हर अलाप में एक दर्द। उन्होंने दिखाया कि दुख भी कला बन सकता है, और कला भी इबादत। ग़ज़लों के संसार में आज भी जब कोई दर्द भरी धुन छेड़ता है, तो हवा में उनका नाम तैरता है—बेगम अख्तर, मल्लिका-ए-ग़ज़ल।
भारतीय शास्त्रीय संगीत और विशेष रूप से ग़ज़ल गायकी की दुनिया में, बेगम अख़्तर (जिन्हें ‘मल्लिका-ए-ग़ज़ल’ के नाम से जाना जाता है) का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उनकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश थी जो सीधे रूह को छू जाती थी, और उनकी गायकी में दर्द, मोहब्बत, और ज़िंदगी के हर रंग का समावेश था। अपनी कला के लिए उन्हें अपार सम्मान मिला, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी के कई पहलू ऐसे भी रहे जो पर्दे के पीछे रहे या जिन पर कम ही चर्चा हुई। 800 शब्दों के इस लेख में, हम बेगम अख़्तर, जिनका मूल नाम अख़्तरी बाई फ़ैज़ाबादी था, के जीवन के कुछ ऐसे ही अनछुए और कम ज्ञात पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे।
आरंभिक जीवन और पहचान की तलाश
उनका संगीत प्रशिक्षण दिग्गज उस्तादों की देखरेख में हुआ, जिनमें उस्ताद अता मोहम्मद खान और बाद में उस्ताद अब्दुल वाहिद खान और उस्ताद झंडे खान शामिल थे। इन उस्तादों ने उन्हें ठुमरी, दादरा और ग़ज़ल की गहरी समझ दी। यह कम ही ज्ञात है कि बेगम अख़्तर ने अपने करियर की शुरुआत में एक शास्त्रीय गायिका के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन तत्कालीन समाज में एक महिला कलाकार के लिए यह राह अत्यंत कठिन थी।
सिनेमा और सामाजिक द्वंद्व
बेगम अख़्तर के जीवन का एक महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चित पहलू उनका सिनेमा करियर है। 1930 और 1940 के दशक के दौरान, उन्होंने कई फ़िल्मों में काम किया और गाया भी। उनकी फ़िल्मों में ‘रोटी’ (1942), ‘नसीब का चक्कर’, और ‘दाना पानी’ शामिल हैं। फ़िल्मों में काम करने का निर्णय उनकी आर्थिक मजबूरी और अपनी कला को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने की इच्छा का परिणाम था। हालांकि, एक प्रतिष्ठित ‘तवायफ़’ पृष्ठभूमि से आने के कारण, फ़िल्म उद्योग में भी उन्हें कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। इस दौर में उनकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग ने उन्हें घर-घर तक पहुंचाया, लेकिन उनके दिल में हमेशा शुद्ध शास्त्रीय और ग़ज़ल गायन की चाहत बनी रही।
वैवाहिक जीवन और संगीत से अलगाव
1945 में, अख़्तरी बाई ने लखनऊ के एक प्रसिद्ध बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी की। यह उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा मोड़ था। शादी के बाद, उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए संगीत को अलविदा कह दिया। यह उनके जीवन का सबसे दर्दनाक और कम चर्चा वाला पहलू है। कला से इस तरह का अलगाव उनकी आत्मा के लिए असहनीय साबित हुआ। इश्तियाक अहमद अब्बासी एक प्रतिष्ठित परिवार से थे और उनकी इच्छा थी कि बेगम अख़्तर एक सामान्य गृहस्थ जीवन अपनाएँ, जिससे उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान मिले।
बेगम अख़्तर ने लगभग पाँच वर्षों तक संगीत से दूरी बनाए रखी। यह दौर उनके लिए अत्यंत कठिन रहा और माना जाता है कि इस अलगाव के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएँ (जैसे अवसाद और अनिद्रा) होने लगीं। डॉक्टरों और उनके शुभचिंतकों ने उन्हें सलाह दी कि अगर उन्हें स्वस्थ रहना है, तो उन्हें अपनी कला, यानी संगीत की ओर लौटना होगा। इस सलाह को मानते हुए, और अपने पति की सहमति से, उन्होंने मंच पर वापसी की, और इस वापसी ने ही उन्हें ‘बेगम अख़्तर’ के रूप में एक अमर पहचान दी।
एक फ़कीर कलाकार की आत्मा
बेगम अख़्तर की निजी ज़िंदगी में अकेलापन और उदासी हमेशा मौजूद रही, जो उनकी गायकी में भी झलकता था। उनकी ग़ज़लें अक्सर आशिक़ी, जुदाई, और ज़िंदगी के फ़ानीपन की बात करती थीं। यह सिर्फ़ गायन नहीं था; यह उनके अपने अनुभवों का निचोड़ था।
उनके बारे में एक और कम ज्ञात बात यह है कि वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक फ़कीर कलाकार की तरह जीती थीं। पैसा और शोहरत होने के बावजूद, वह सादगी से रहती थीं और उनका जीवन पूरी तरह से उनकी कला को समर्पित था। वह अपने घर आने वाले शिष्यों और मेहमानों का खुले दिल से स्वागत करती थीं, और अक्सर अपने प्रिय ग़ज़लों को गाकर उन्हें सुनाया करती थीं। वह एक ऐसे युग की अंतिम कड़ी थीं जहाँ कलाकार अपनी कला को साधना मानते थे, न कि महज़ एक पेशा।
विरासत और अंतिम यात्रा
बेगम अख़्तर ने 30 अक्टूबर 1974 को अहमदाबाद में एक कंसर्ट के दौरान अंतिम साँस ली। यह उनके जीवन की एक दुखद विडंबना थी कि उनकी मौत मंच पर, अपने श्रोताओं के सामने, संगीत की सेवा करते हुए हुई। उनकी अंतिम रिकॉर्डिंग, जिसमें उनकी आवाज़ हमेशा की तरह दर्द और गहराई से भरी थी, उनकी अमर कला का एक प्रमाण है।
बेगम अख़्तर का जीवन संघर्ष, त्याग और कला के प्रति अटूट समर्पण की एक कहानी है। ‘मल्लिका-ए-ग़ज़ल’ बनने के लिए उन्होंने सामाजिक बहिष्कार झेला, अपनी कला को त्यागने की कोशिश की, और फिर उसे फिर से अपनाया। उनके जीवन के ये अनछुए पहलू हमें बताते हैं कि जिस दर्द को वह अपनी ग़ज़लों में बयां करती थीं, वह महज़ एक प्रस्तुति नहीं, बल्कि उनकी अपनी ज़िंदगी का सच्चा अनुभव था।
मल्लिका-ए-ग़ज़ल बेगम अख़्तर की आवाज़ में एक ऐसा दर्द और जादू था, जो उनकी गायी हर ग़ज़ल को अमर कर देता था। उनकी निजी ज़िंदगी के गहरे अनुभव और संगीत के प्रति उनका अटूट समर्पण उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के पीछे की असली कहानियाँ हैं।
यहाँ उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध ग़ज़लों के पीछे की कहानियों और उनसे जुड़े रोचक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है:
1. “ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया” (शकील बदायूँनी)
यह ग़ज़ल बेगम अख़्तर के सबसे प्रतिष्ठित और हृदयस्पर्शी कलामों में से एक है, जो उनकी गायकी की पहचान बन गया।
कहानी: एक रेलवे स्टेशन पर जन्म
इस ग़ज़ल की रचना और बेगम अख़्तर द्वारा इसे अपनाए जाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है:
शायर से मुलाक़ात: एक बार बेगम अख़्तर बम्बई (अब मुंबई) में एक संगीत जलसे में शरीक होने के बाद ट्रेन से लखनऊ लौट रही थीं। विक्टोरिया टर्मिनस (VT) स्टेशन पर, शायर शकील बदायूँनी उनसे मिले। शकील बदायूँनी तब संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी शायरी में कमाल की गहराई थी। शकील ने जल्दबाज़ी में एक कागज़ का टुकड़ा बेगम अख़्तर को यह अनुरोध करते हुए थमाया कि वह इसे गाएँ। कागज के टुकड़े पर उन्होंने यह नई ग़ज़ल लिखी थी,। बेगम अख़्तर ने उस कागज़ को बिना देखे ही अपने बटुए में रख लिया। ट्रेन के सफ़र के दौरान, बेगम अख़्तर को अचानक वह कागज़ याद आया। उन्होंने ग़ज़ल पढ़ी और उसके बोलों की गहराई से इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने राग भैरवी में तुरंत उसकी धुन (कंपोज़िशन) तैयार कर ली। लखनऊ पहुँचकर, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो (AIR) पर अपने कार्यक्रम में सबसे पहले इसी ग़ज़ल को पेश किया। जैसे ही उन्होंने ये पंक्तियाँ गाईं: “ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया…” यह ग़ज़ल रातों-रात अविस्मरणीय बन गई और शकील बदायूँनी को भी नई पहचान मिली।
2. “वो जो हम में तुम में क़रार था” (मोमिन ख़ाँ मोमिन)
यह एक क्लासिक ग़ज़ल है जो उर्दू शायरी के महान शायर मोमिन ख़ाँ मोमिन की है। बेगम अख़्तर की आवाज़ ने इसे अमरता प्रदान की। यह ग़ज़ल बेगम अख़्तर के जीवन के उस दौर से जुड़ी हुई महसूस होती है, जब उन्होंने अपने पति इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी करने के बाद सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए पाँच साल तक गाना छोड़ दिया था। कला से यह अलगाव उनके लिए अत्यंत कष्टदायक था, और वह बीमार रहने लगी थीं। एक कलाकार के लिए उसकी कला से दूर रहना, जैसे मछली का पानी के बिना रहना है।
इस ग़ज़ल के बोल, “वो जो हम में तुम में क़रार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो…”, विरह, पुरानी यादों, और टूटे वादों का एक सुंदर चित्रण हैं। बेगम अख़्तर की आवाज़ में वह उदासी और तड़प उनके अपने जीवन के खोए हुए वर्षों और संगीत के प्रति उनके प्रेम की वापसी की कहानी कहती है। जब उन्होंने 1949 में रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वापसी की, तो उनकी गायकी में एक नई, गहरी कशिश आ गई थी, जिसकी अभिव्यक्ति इस ग़ज़ल में साफ झलकती है।
3. “ये न थी हमारी क़िस्मत कि विसाल-ए-यार होता” (मिर्ज़ा ग़ालिब)
मिर्ज़ा ग़ालिब की इस कालजयी ग़ज़ल को बेगम अख़्तर ने अपनी जादुई आवाज़ से एक नया आयाम दिया।
कहानी: शास्त्रीय विरासत का सम्मान
बेगम अख़्तर हमेशा ग़ज़ल को शास्त्रीय संगीत के समान ऊँचा दर्जा दिलाना चाहती थीं।
शास्त्रीय आधार: हालाँकि उन्हें ‘तवायफ़’ संस्कृति से आने के कारण अक्सर सामाजिक संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पास ठुमरी, दादरा और खयाल की मजबूत शास्त्रीय पृष्ठभूमि थी। ग़ालिब की यह ग़ज़ल, अपने गहरे दार्शनिक और दर्द भरे बोलों के कारण, बेगम अख़्तर को अपनी शास्त्रीय गायकी का बेहतरीन मिश्रण पेश करने का मौका देती थी। ग़ज़ल के बोल—”ये न थी हमारी क़िस्मत कि विसाल-ए-यार होता… विफलता, भाग्य और निराशा की भावना व्यक्त करते हैं, जो बेगम अख़्तर की निजी ज़िंदगी (बचपन का संघर्ष, एक बेटी को खोना, और समाज द्वारा कला को नीचा दिखाना) के दर्द से मेल खाती थी। जब वह इस ग़ज़ल को गाती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे वह ग़ालिब के दर्द को अपनी आत्मा में उतारकर प्रस्तुत कर रही हैं, जिससे यह महज़ गायन न रहकर एक मार्मिक आत्म-निवेदन बन जाता था।
बेगम अख़्तर की हर ग़ज़ल महज़ एक गाना नहीं थी, बल्कि उनकी ज़िंदगी के संघर्षों, प्रेम, विरह, और कला के प्रति उनके गहरे समर्पण का एक भावनात्मक दस्तावेज थी।