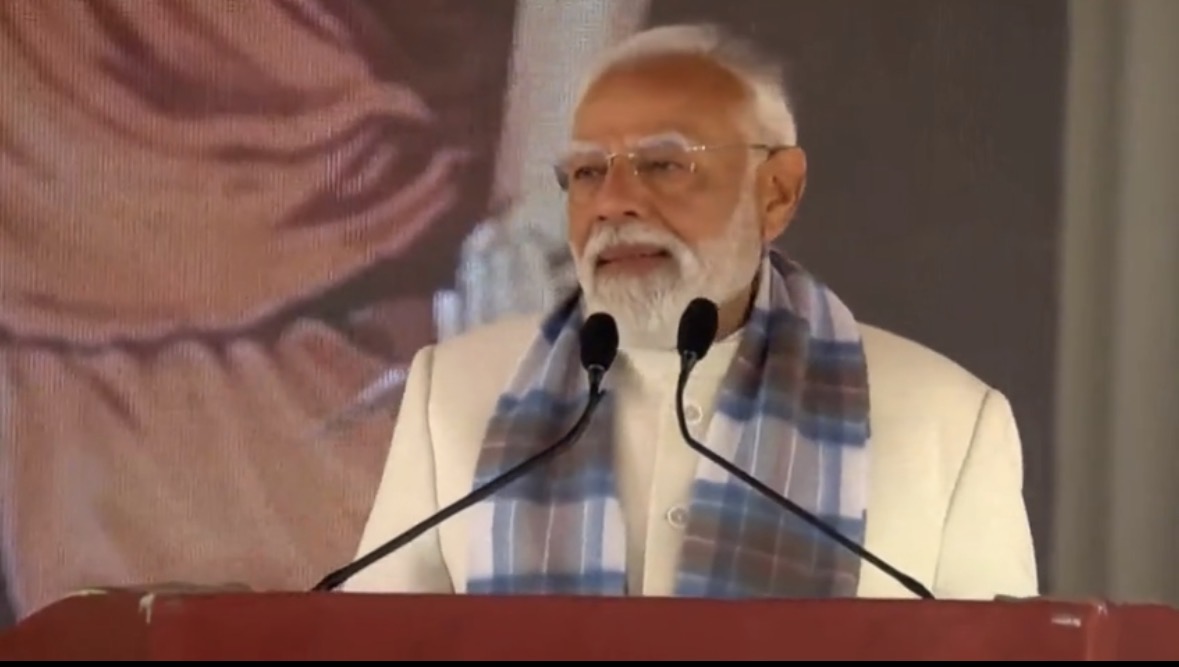खूंटी, 14 जनवरी (हि.स.)। बिहार के गयाजी स्थित सीताकुंड निवासी चंदन मेहता (18 ) और जहानाबाद जिले के 17 वर्षीय किशोर अमित सोनी इन दिनों अपने अनोखे और साहसिक भारत दर्शन को लेकर चर्चा में हैं। दोनों युवक गत 16 नवंबर 2025 को स्केटिंग करते हुए संपूर्ण भारत यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा का उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने के साथ-साथ अपने विचारों को देशभर में लोगों तक पहुंचाना है।
चंदन और अमित स्केटिंग के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों और धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। इस क्रम में वे ओडिशा के जगन्नाथ पुरी पहुंचे, जहां दर्शन-पूजन के बाद अयोध्या धाम जाने के लिए रवाना हुए। अयोध्या जाने के दौरान दोनों बुधवार को तोरपा पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनके साहस और संकल्प की सराहना की और स्वागत किया।
यात्रा के दौरान दोनों युवकों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की है। इसके लिए वे जगह-जगह लोगों से संवाद कर जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को मजबूत करना आज के समय की आवश्यकता है।
चंदन और अमित का लक्ष्य देशभर के सभी 52 शक्तिपीठों का दर्शन करना है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि अब तक वे 14 शक्तिपीठों के दर्शन कर चुके हैं। उनका कहना है कि यह यात्रा केवल धार्मिक दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की विविध संस्कृति, परंपरा और लोगों से जुड़ने का एक माध्यम भी है।
यात्रा में आने वाली चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर दोनों ने बताया कि स्केटिंग करते हुए लंबी दूरी तय करना आसान नहीं है, लेकिन उनका उत्साह और आस्था उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। रात के समय वे प्रायः किसी मंदिर परिसर में ठहरते हैं और वहीं से अगली सुबह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।
भारत दर्शन में कुल कितना समय लगेगा, इस प्रश्न पर दोनों का कहना है कि इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं है। उनका लक्ष्य समय की सीमा नहीं, बल्कि संकल्प की पूर्ति है। जब तक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, यात्रा जारी रहेगी।
तोरपा में लोगों ने इन युवाओं के जज्बे को सलाम करते हुए उनके सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की। उन्होंने बताया कि वे प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं और यात्रा के समापन पर वे गुरु के दर्शन करेंगे।