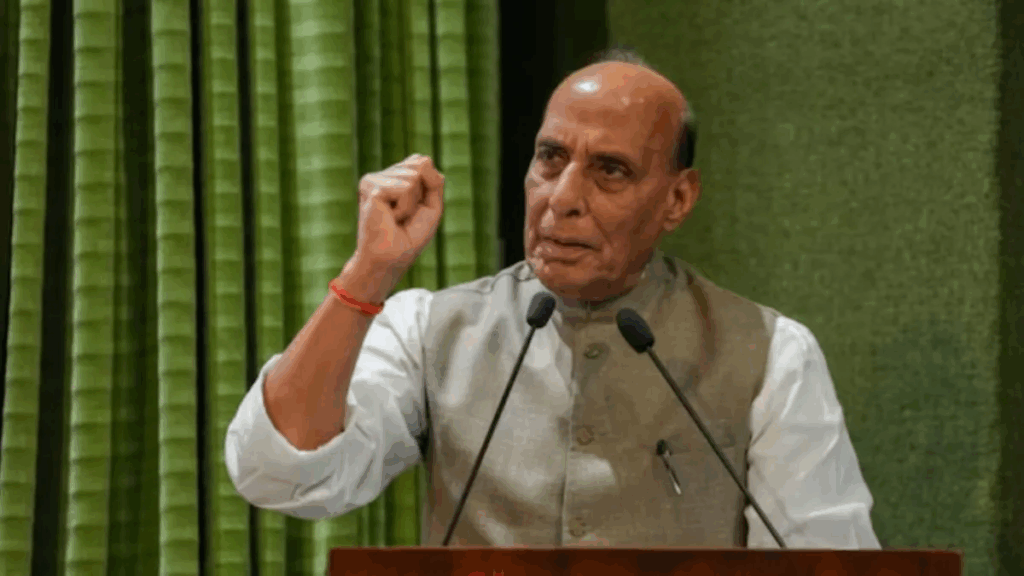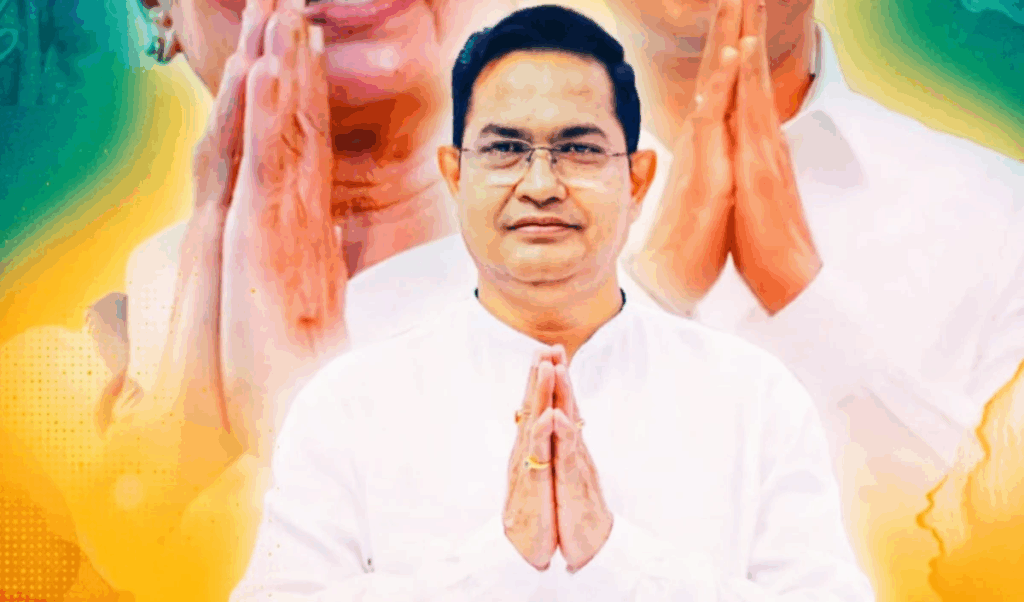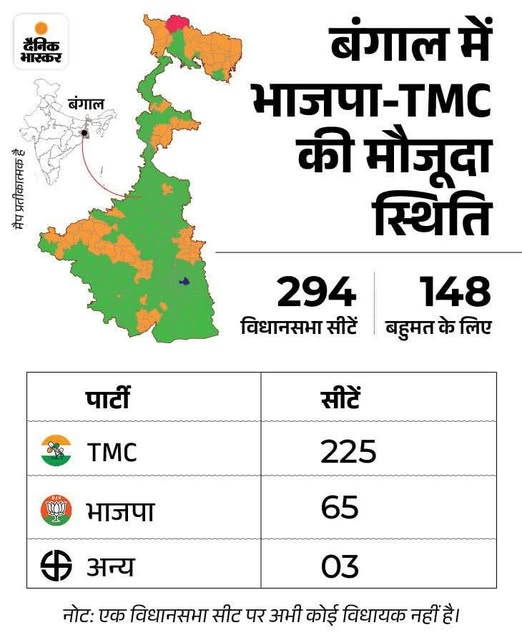व्यक्ति की स्वतंत्रता, पारिवारिक मर्यादा और एक त्रासदी का गहन सामाजिक विश्लेषण
“स्वतंत्रता और परंपरा—दोनों अपने-अपने स्थान पर सही, पर जब टकराते हैं तो सबसे पहले टूटता है एक सामान्य परिवार। कानून अपना काम करता है, समाज अपनी जिद पर अड़ा रहता है, और बीच में पिस जाता है वह घर जिसने न विद्रोह किया, न अपराध—फिर भी वही सबसे बड़ा शिकार बन जाता है।”
– डॉ. प्रियंका सौरभ
भारत जैसे विशाल और विविध सामाजिक ढाँचे वाले राष्ट्र में व्यक्ति के अधिकार और समाज की सामूहिक मर्यादाएँ एक-दूसरे से लगातार टकराती रहती हैं। संविधान व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार देता है, लेकिन सामाजिक परम्पराएँ यह स्वीकार नहीं कर पातीं कि कोई लड़की या लड़का परिवार की इच्छा और बिरादरी की मान्यताओं से अलग कोई जीवननिर्णय ले। यह संघर्ष नया नहीं है, लेकिन आज की जमीनी हकीकत में इसका तनाव कहीं अधिक विकराल रूप ले चुका है।
हाल ही की एक त्रासदी में यही टकराव खुलकर सामने आया, जब एक युवती ने अपने ही गाँव के युवक से विवाह कर लिया—ऐसा विवाह जो पूरी तरह कानूनी था, लेकिन समाज की दृष्टि में सर्वथा अस्वीकार्य। सामाजिक विरोध, पंचायत की मनाही, परिवार की पीड़ा और प्रतिष्ठा के दबाव के बीच लड़की शहर चली गई थी, पर कुछ समय बाद वापस अपने ही पैतृक गाँव में बहू बनकर लौट आई। यही वापसी समाज को चुनौती की तरह दिखाई दी और परिवार पर अत्यन्त तीव्र मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा। वही दबाव परिस्थितियों को उस कगार तक ले गया जहाँ भाई ने अपनी ही बहन की हत्या कर दी। इस एक क्षण ने न केवल एक जीवन छीना, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया।
यह घटना सिर्फ मानवता पर एक चोट नहीं है, यह एक ऐसा दर्पण भी है जिसमें हम अपने समय की सबसे बड़ी विडंबना को साफ देख सकते हैं—कानून कुछ कहता है, समाज कुछ और। व्यक्ति की स्वतंत्रता एक दिशा में जाती है, जबकि परंपराएँ दूसरी दिशा में खींचती हैं। इन दोनों के बीच जो परिवार खड़ा होता है, वह अक्सर दोनों ओर से घायल होता है। कानून वयस्कता की उम्र तय कर देता है, पर वह ग्रामीण समाज की संवेदनात्मक संरचना, परिवार की प्रतिष्ठा, और सामुदायिक दबाव को नहीं समझता। वहीं समाज स्वतंत्रता के अधिकार को “अवज्ञा” या “विद्रोह” की तरह देखता है और परिवार पर ऐसी जिम्मेदारियाँ डाल देता है जिन्हें निभाना असंभव है।
परिवार ही इस संघर्ष का सबसे बड़ा पीड़ित बनता है। बेटी का गांव छोड़कर जाना, रिश्तेदारों की टिप्पणियाँ, पंचायत का दबाव, सामाजिक प्रतिष्ठा का संकट—ये सभी घटनाएँ एक घर को भीतर से हिलाकर रख देती हैं। कानून परिवार से लड़की को स्वीकार करने का संदेश देता है, जबकि समाज उसे अस्वीकार करने का दबाव डालता है। ये दोनों ताकतें परिवार को दो हिस्सों में चीर देती हैं—एक हिस्सा जिसे मन ने स्वीकार कर लिया है, और दूसरा हिस्सा जिसे समाज स्वीकार नहीं करने देता। ऐसे में विवेक धुंधला पड़ जाता है और भावनाएँ निर्णयों पर हावी होने लगती हैं।
इस घटना का सबसे भयावह पहलू यह था कि सोशल मीडिया पर 95 प्रतिशत टिप्पणियाँ इस हत्या को “सही” ठहरा रही थीं। यह केवल कुछ व्यक्तियों की राय नहीं, बल्कि समाज में पनप रही एक खतरनाक सामूहिक सोच का संकेत है। जब कोई समाज अपनी भावनाओं और परंपराओं के दबाव में हत्या जैसे अपराध को भी न्याय मानने लगे, तो यह किसी भी सभ्य व्यवस्था के लिए अत्यन्त गंभीर स्थिति है। कानून की शक्ति तभी तक है जब तक समाज उसे नैतिक समर्थन देता है। जब समाज हिंसा को नैतिक ठहराने लगे, कानून कमजोर नहीं, बल्कि अप्रासंगिक हो जाता है। और यही स्थिति किसी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है।
विवाह की स्वतंत्रता का प्रश्न भी इस घटना में नए दृष्टिकोण से उभरता है। भारतीय कानून मानता है कि 18 और 21 वर्ष की उम्र में व्यक्ति परिपक्व और स्वतंत्र निर्णय लेने योग्य होता है। पर क्या वास्तव में यह उम्र जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बिना परिवार के अनुभव, बिना सामाजिक समझ, बिना भविष्य की जिम्मेदारियों को समझे लेने के लिए पर्याप्त है? भारतीय परिवार व्यवस्था में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मामला नहीं होता, यह दो परिवारों, रिश्तों और समाजों का मामला होता है। ऐसे में कम आयु में किया गया आवेगपूर्ण निर्णय केवल व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार को प्रभावित करता है।
यही कारण है कि कई लोग तर्क देते हैं कि विवाह के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक होनी चाहिए—कम से कम 30 वर्ष की आयु तक। यह विचार सामाजिक अनुभवों से उत्पन्न है, पर संवैधानिक दृष्टि से कठिन है। यदि माता-पिता की सहमति अनिवार्य कर दी जाए, तो यह युवाओं पर अत्यधिक दबाव और कई मामलों में दमन को भी जन्म दे सकता है। फिर भी यह भी सच है कि परिवार से विमुख होकर किए गए विवाहों के परिणामों का सबसे बड़ा बोझ परिवारों को ही उठाना पड़ता है। यह द्वंद्व इतना गहरा है कि कोई भी पक्ष न पूरी तरह सही ठहराया जा सकता है, न पूरी तरह गलत।
समाज अक्सर कहता है कि लड़की ने “परिवार की कई हत्याएँ कर दीं”—यह भाषा कानूनी नहीं, बल्कि भावनात्मक है। कानून भावनात्मक मृत्यु को अपराध नहीं मान सकता। पर परिवार इसे वास्तविक समझता है क्योंकि वे इसे प्रत्यक्ष जीते हैं। यही वह खाई है जिसे पाटना सबसे कठिन है। कानून कहता है निर्णय व्यक्तिगत है; समाज कहता है निर्णय सामूहिक है। और इन्हीं दो कथनों के बीच वह परिवार टूट जाता है जिसके इर्द-गिर्द इस तरह की घटनाएँ जन्म लेती हैं।
इस मामले में सबसे अधिक नुकसान उसी परिवार का हुआ जिसने न अपराध चुना, न विद्रोह। लड़की की जान चली गई, भाई का जीवन जेल में समाप्त, माता-पिता ने एक बेटी और एक बेटे दोनों को खो दिया, घर की आर्थिक-सामाजिक नींव हिल गई, बच्चों का भविष्य अनिश्चित हो गया। जबकि समाज के लिए यह महज चर्चा का विषय रह गया, और सरकार के लिए सिर्फ एक केस फाइल।
प्रश्न यह है कि सरकार क्या कर सकती है? भागकर विवाह पर रोक समाधान नहीं है, पर इस प्रक्रिया में सुधारों की आवश्यकता है। विवादित विवाह से पहले अनिवार्य परामर्श, परिवार–युवा मध्यस्थता, पंचायतों के अधिकारों पर स्पष्ट सीमा, और स्कूल-कॉलेजों में सामाजिक जिम्मेदारी की शिक्षा—ये सभी कदम जरूरी हैं। न्यायिक और प्रशासनिक संस्थाओं को भी परिवार की सामाजिक पीड़ा को समझने की आवश्यकता है।
फिर भी सरकार और कानून दोनों अकेले समस्या हल नहीं कर सकते। जब तक समाज संवाद को हिंसा से ऊपर नहीं रखेगा, जब तक परिवार गुस्से से ऊपर संवाद को नहीं चुनेगा, और जब तक युवा आवेग को निर्णय का आधार बनाना बंद नहीं करेंगे—तब तक ऐसी त्रासदियाँ रुकने वाली नहीं हैं।
आज़ादी का अर्थ स्वेच्छाचार नहीं, और परंपरा का अर्थ दमन नहीं। दोनों के बीच संतुलन ही सभ्यता का आधार है।
अंततः यही समझना होगा कि कानून और समाज की लड़ाई में जीत किसी की नहीं होती—हार हमेशा एक इंसान और एक परिवार की ही होती है।
-प्रियंका सौरभ
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,