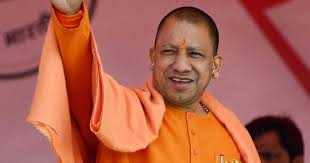वीबी-जी राम जी पर ग्राम चौपालों में जनसंवाद करेगी भाजपा
लखनऊ, 13 जनवरी (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी वीबी-जी राम जी अधिनियम के बारे में जनता को बताने के लिए लेकर गांव, गली, मजरो, चौपालों पर पहुंचकर जनसंवाद करेगी। मंगलवार को केन्द्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति में लखनऊ के इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 पर संवाद आयोजित हुआ।
इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि विकसित भारत वीबी-जी राम जी मजदूर किसान और गांव के विकास का मंत्र है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार का अंत है। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी से भ्रष्टाचार खत्म होगा गांव का विकास होगा ग्रामीण क्षेत्र में नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होंगे। जब गांव का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा और देश विकसित भारत की ओर तेजी से अग्रसर होगा।
पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले 11 वर्षों में ग्रामीण भारत की दशा और दिशा दोनों को बदलने का ऐतिहासिक कार्य किया है। आज देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, यह केवल आंकड़ा नहीं बल्कि नीतियों की सफलता और गरीब के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि हर गरीब को रोजगार मिले, उसकी गरिमा का सम्मान हो और विकास का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को विकसित भारत और भगवान श्रीराम के नाम से इतनी नफरत क्यों है? कांग्रेस चाहे कितनी भी साजिशें कर ले, भारत 2047 तक विकसित भारत बनकर रहेगा। इस संकल्प को कोई नहीं रोक सकता।
श्री चौधरी ने कहा कि वीबी-जी राम जी के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को हर वर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। वन क्षेत्रों में कार्य करने वाले कामगारों को अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार मिलेगा। काम के दिन बढ़ेंगे और साथ ही मजदूरी का भुगतान भी पहले से कहीं अधिक तेज़ होगा। मनरेगा के विपरीत, इस नए कानून में हर सप्ताह भुगतान का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कार्यशाला में उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे पार्टी संगठन की योजनानुसार गांव-गांव व जन-जन तक वीबी-जी राम जी से आमजन को मिलने वाले लाभ के बारे में बताकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और झूठ का पर्दाफाश करें।