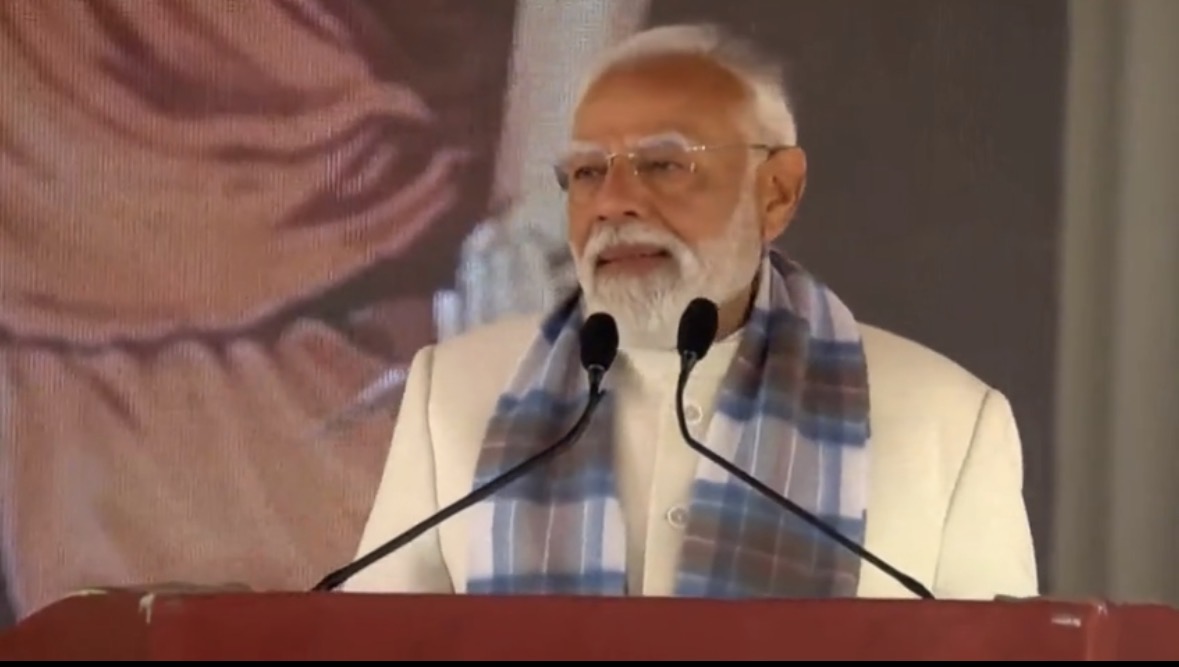नई दिल्ली, 14 जनवरी (हि.स.)। घरेलू सर्राफा बाजार में हाजिर चांदी की कीमत में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। देश के अलग-अलग हिस्सों में ये चमकीली धातु आज पांच हजार रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 20,300 रुपये प्रति किलोग्राम तक महंगी हो गई है। दिल्ली में ये चमकीली धातु पौने तीन लाख के स्तर को पार कर गई है। वहीं चेन्नई और हैदराबाद में चांदी जोरदार छलांग लगा कर तीन लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर के काफी करीब पहुंच गई है। भाव में आई इस तेजी के कारण देश के अलग अलग सर्राफा बाजारों में आज चांदी 2,74,900 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 2,97,900 रुपये प्रति किलोग्राम तक के भाव पर बिक रही है।
दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी आज पांच हजार रुपये प्रति किलोग्राम उछल गई है, जिसके कारण ये चमकीली धातु आज 2,75,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। इसी तरह मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता में चांदी 2,74,900 रुपये के भाव पर कारोबार कर रही है। जबकि जयपुर, सूरत और पुणे में चांदी 2,75,200 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है।
वहीं बेंगलुरु में चांदी 2,75,400 रुपये के स्तर पर और पटना तथा भुवनेश्वर में 2,75,000 प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। इसके अलावा हैदराबाद में चांदी 20,100 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी के साथ 2,97,400 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। देश में चांदी की सबसे अधिक कीमत आज भी चेन्नई में है, जहां ये चमकीली धातु आज 20,300 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी होकर 2,97,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है।
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरनेशनल से लेकर डोमेस्टिक मार्केट तक चांदी को लेकर पॉजिटिव नोट्स नजर आ रहे हैं। खासकर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड और ईरान को लेकर जो संकेत दिए हैं, उससे अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हलचल की स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही जनवरी के दूसरे पखवाड़े में चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड में भी और तेजी आने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में चांदी के भाव में आगे भी तेजी जारी रहने की उम्मीद बनी हुई है।
कैपेक्स गोल्ड एंड इनवेस्टमेंट्स के सीईओ राजीव दत्ता का कहना है कि इस साल घरेलू बाजार में अब तक चांदी की कीमतों में 200 प्रतिशत से अधिक की तेजी आ चुकी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंची हुई है। लंदन सिल्वर मार्केट में आज चांदी का हाजिर भाव 90.95 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था। जियो पॉलिटिकल टेंशन और इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही है।
राजीव दत्ता के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी से जुड़े उद्योगों में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। और तो और, सेफ इनवेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी चांदी में निवेश बढ़ा है। खासकर, सिल्वर ईटीएफ में लगातार इनफ्लो होता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगर बाजार की स्थिति में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ और चांदी की मांग में मजबूती बनी रही, तो आने वाले दिनों में इसकी कीमत 100 डॉलर (करीब 9030 रुपये) प्रति औंस के स्तर तक भी पहुंच सकती है।