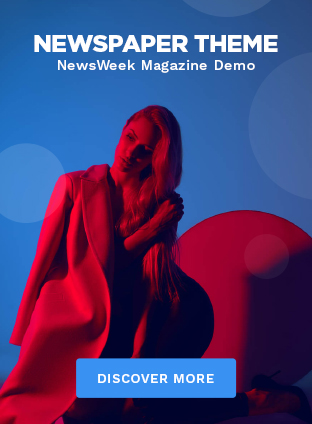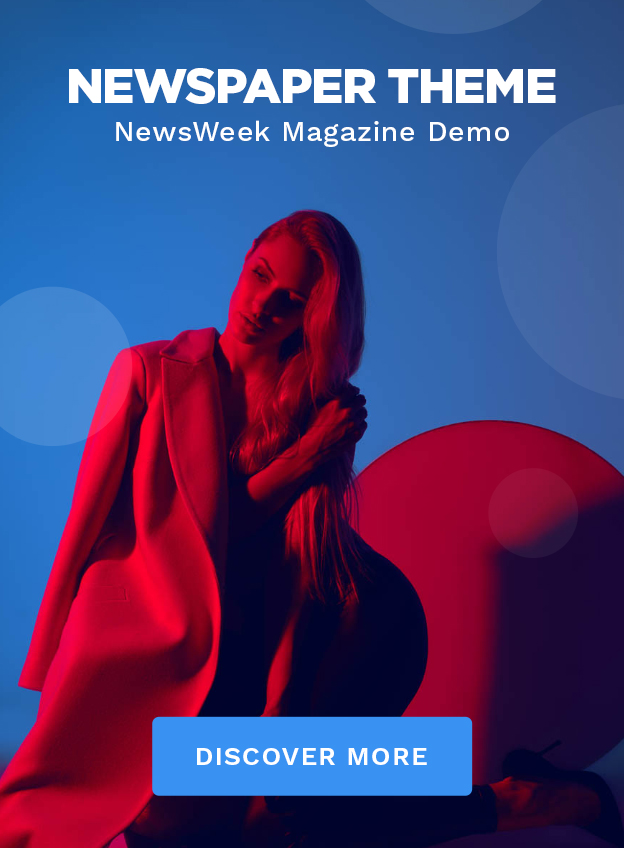आज का समाज उपभोक्ता संस्कृति का गुलाम बन चुका है। लोग जरूरत के लिए नहीं, बल्कि दिखावे के लिए चीजें खरीद रहे हैं। मोबाइल फोन से लेकर कपड़ों तक, हर वस्तु अब पहचान और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई है। “लोग क्या कहेंगे” के डर में लोग कर्ज में डूबते जा रहे हैं। असली जरूरतें पीछे छूटती जा रही हैं और कृत्रिम इच्छाएं आगे बढ़ रही हैं। उपभोक्तावाद का यह जाल धीरे-धीरे इंसान की आत्मा को खाली कर रहा है।
 डॉ. प्रियंका सौरभ
डॉ. प्रियंका सौरभ
हमारा समाज आज विकास की तेज़ रफ़्तार पर तो है, पर दिशा कहीं खो चुका है। पहले इंसान ज़रूरतों के लिए चीज़ें खरीदता था, अब चीज़ें इंसान को खरीद रही हैं। अब बाज़ार केवल सामान नहीं बेचता, वह हमारी पहचान बेचता है। यह हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हम कौन हैं, हमारी औक़ात क्या है, और हमारी असली कीमत कितनी है। आज हर तरफ़ एक अजीब सी होड़ है — दिखावे की, ब्रांड की, और झूठे रुतबे की। लोग अब ज़िंदगी नहीं जी रहे, वे उसे प्रदर्शित कर रहे हैं। हर तस्वीर, हर पोस्ट, हर कपड़े और हर मोबाइल के पीछे एक ही सवाल छिपा होता है – “लोग क्या कहेंगे?”
उपभोक्तावाद यानी कंज़्यूमरिज़्म ने हमारे समाज की नसों में ज़हर की तरह जगह बना ली है। पहले व्यक्ति वस्तु का उपयोग करता था, अब वस्तुएँ व्यक्ति का उपयोग कर रही हैं। ब्रांड अब हमारी ज़रूरतों के नहीं, बल्कि हमारी असुरक्षाओं के सौदागर बन गए हैं। वे हमें यह यक़ीन दिला चुके हैं कि जब तक हमारे पास महंगा मोबाइल, बड़ा घर और इंस्टाग्राम पर दिखाने लायक जीवन नहीं है, तब तक हम अधूरे हैं।
कभी कहा गया था कि “मनुष्य वस्तु का मालिक है”, पर अब वस्तुएँ मनुष्य के मन और मानसिकता की मालिक बन चुकी हैं। ऐप्पल का मोबाइल हो या महंगी कार, इनका उद्देश्य सुविधा नहीं, प्रतिष्ठा बन चुका है। लोग अब पर्दा इसलिए नहीं हटाते कि उन्हें हवा लगे, बल्कि इसलिए हटाते हैं कि तस्वीर अच्छी आए। इज़्ज़त अब चरित्र में नहीं, कैमरे की फ्रेम में दिखती है।
सोशल मीडिया इस उपभोक्ता संस्कृति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। पहले लोग बातें करते थे, अब पोस्ट करते हैं। पहले खुशी आती थी, अब उसे रील में एडिट किया जाता है। पहले त्यौहार मनाए जाते थे, अब दिखाए जाते हैं।
हर लाइक आत्मविश्वास का मापदंड बन गया है, और हर टिप्पणी आत्म-मूल्य का प्रमाण। हम खुद से कम और दूसरों की निगाह से ज़्यादा जीने लगे हैं। कपड़े ब्रांडेड हैं, पर सोच उधार की है; चेहरे चमकते हैं, पर दिल थके हुए हैं।
एक समय था जब गाँव की औरतें पर्दे में रहकर भी मर्यादा और सम्मान की मिसाल होती थीं। आज वही परंपरा इंस्टाग्राम की चमक में खो गई है। अब पर्दा शर्म या संकोच का नहीं, बल्कि फोटोशूट का हिस्सा बन गया है। लोग कहते हैं — “हम तो आधुनिक हैं।” पर यह आधुनिकता नहीं, मानसिक गुलामी है — जहाँ दिखावा आत्म-सम्मान पर भारी पड़ता है।
सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपनी मासिक कमाई का बड़ा हिस्सा केवल इसीलिए ईएमआई में खर्च कर देता है ताकि लोग कह सकें कि उसके पास ‘आइफ़ोन’ है — तो वह उपभोक्ता नहीं, बल्कि उपभोग का शिकार बन चुका है।
फ़ोन वही काम करता है — बात करना, संदेश भेजना, संपर्क बनाए रखना — पर हमारे दिमाग़ ने उसे सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बना लिया है।
बाज़ार हमें यह नहीं बताता कि हमें क्या चाहिए, बल्कि यह तय करता है कि हमें क्या चाहना चाहिए। विज्ञापन इतने मनोवैज्ञानिक हो चुके हैं कि वे पहले हमारे भीतर कमी का एहसास जगाते हैं, फिर उसी कमी का समाधान बेचते हैं।
यह एक मानसिक व्यापार है — पहले असंतोष पैदा करो, फिर संतोष बेचो। मोबाइल कंपनियाँ कहती हैं — “हमारा फ़ोन आपकी पहचान है।” धीरे-धीरे यही सोच हमारी आत्मा तक उतर गई है। हमारी पहचान, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान — सब अब ब्रांड वैल्यू में बदल चुके हैं।
जब मूल्य वस्तु में बदल जाते हैं, तो रिश्ते भी सौदे में बदल जाते हैं। आज लोग उपहार नहीं, ब्रांडेड चीज़ें देते हैं।
शादी अब संस्कार नहीं, सामाजिक प्रदर्शन बन गई है।
त्योहार अब भावना नहीं, फोटो सेशन बन चुके हैं।
यह सब मिलकर हमारी संवेदनाओं को खोखला और नकली बना रहे हैं।
पहले माता-पिता बच्चों को सिखाते थे — “कपड़े से नहीं, कर्म से पहचान होती है।” अब बच्चे कहते हैं — “माँ, वही ब्रांड चाहिए जो मेरे दोस्त के पास है।” यही वह पल होता है जहाँ संस्कार हार जाते हैं और बाज़ार जीत जाता है। कई लोग कहते हैं — “हम तो ईएमआई पर खरीद रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है?” पर फर्क यह है कि अब आप उस चीज़ के मालिक नहीं, बल्कि वह चीज़ आपकी जेब और मानसिक शांति की मालिक बन गई है। ईएमआई केवल किस्त नहीं, एक अदृश्य जंजीर है जो आत्मसंतोष को बाँध लेती है।
महंगी वस्तुएँ कुछ पलों की खुशी देती हैं, पर धीरे-धीरे वही बोझ बन जाती हैं।
मध्यवर्गीय समाज आज सबसे ज़्यादा इस झूठी प्रतिष्ठा की होड़ में फँसा हुआ है। वह अपनी असल ज़रूरतें भूल चुका है, और दिखावे की दुनिया में जी रहा है। वह “कैसा दिखता हूँ” में उलझ गया है, “मैं क्या हूँ” यह भूल गया है। दिखावे की संस्कृति ने केवल जेब नहीं, नैतिकता भी खाली कर दी है।
अब लोग दूसरों की नज़रों में अच्छे दिखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कोई अपनी निजता बेच रहा है, कोई झूठे रिश्ते दिखा रहा है, तो कोई सस्ती लोकप्रियता के लिए मर्यादा छोड़ रहा है। जहाँ कभी पर्दा सम्मान का प्रतीक था, आज वही पर्दा फोटोशूट की सजावट बन गया है।
अब सच्चाई दिखाना पुराना चलन माना जाता है। जो दिखता है वही बिकता है — यही आज की दुनिया का नारा है। पर जो बिकता है, वह सदा टिकता नहीं। दिखावे की चमक थोड़े समय की होती है, पर सच्चाई की रोशनी स्थायी होती है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है — आपका आत्मसम्मान। उसे कोई बाज़ार, कोई सेल, कोई ऑफर नहीं खरीद सकता। जरूरतें पूरी कीजिए, लेकिन इच्छाओं को समझदारी से सीमित कीजिए। फ़ोन काम के लिए हो, पहचान के लिए नहीं। सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का माध्यम बने, आत्ममूल्य का मापदंड नहीं।
मर्यादा का अर्थ बंदिश नहीं, बल्कि अपनी असल पहचान है।
दिखावे के शोर में सादगी की आवाज़ ही सबसे प्रभावशाली होती है। अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच और ख़रीददारी की मानसिकता बदलनी होगी।
यह समय हमसे सवाल करता है — क्या हम अपने मालिक हैं या बाज़ार के गुलाम? क्या हम दिखावे की दौड़ से निकलकर सच्चे आत्मसंतोष की राह पकड़ सकते हैं? सवाल आसान है, पर जवाब कठिन। क्योंकि यह लड़ाई पैसों की नहीं, मानसिकता की है। यह तय करेगा कि हम तकनीक और चमक के बीच रहकर भी इंसान बने रह सकते हैं या नहीं।
फ़ोन चाहे किसी का भी हो, बात इंसानियत की होनी चाहिए। जब तक हम अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा अपनी असलियत को महत्व नहीं देंगे, तब तक हम बाज़ार के आईने में अपने ही नकली प्रतिबिंब को देखते रहेंगे। समाज तब आगे बढ़ता है जब वस्तुएँ साधन बनें, साध्य नहीं।
अब समय है कि हम खुद को ब्रांड के उपभोक्ता नहीं, मूल्यों के रक्षक बनाएं। क्योंकि बाज़ार की चमक एक दिन फीकी पड़ जाएगी, पर इंसानियत की रोशनी कभी नहीं।
-प्रियंका सौरभ
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार