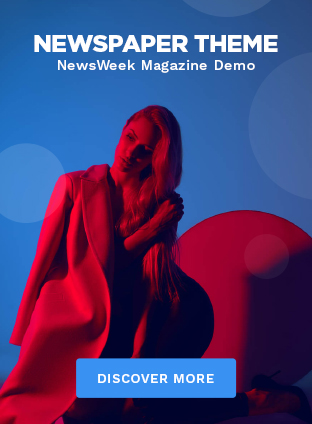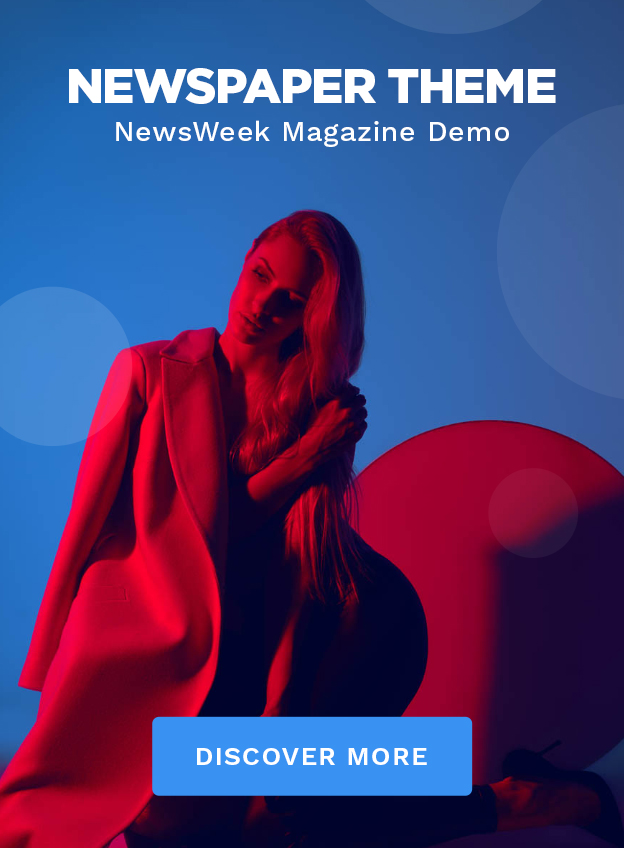“एक वर्दी का मौन:
(पद और प्रतिष्ठा के पीछे छिपी पीड़ा का मौन विस्फोट — हरियाणा के एडीजीपी वाई.एस. पूरण की आत्महत्या समाज के संवेदनहीन होते ढांचे पर गहरा सवाल उठाती है।)
पूरन कुमार की आत्महत्या केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे की विफलता का प्रतीक है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान न देना, लगातार दबाव और अकेलापन, संवेदनशील अधिकारियों को भीतर से तोड़ देता है। हमें अपने प्रशासनिक तंत्र में नियमित काउंसलिंग, गोपनीय सहायता और संवाद की व्यवस्था करनी होगी। समाज और मीडिया को भी संवेदनशील होना चाहिए, सनसनीखेज़ी की बजाय सहानुभूति और सुधार पर ध्यान देना चाहिए। केवल इसी तरह हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोक सकते हैं और अपने अधिकारियों को उनका सम्मान और सुरक्षा दिला सकते हैं।
 डॉ. प्रियंका सौरभ
डॉ. प्रियंका सौरभ
कभी-कभी किसी घटना की ख़बर केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, बल्कि वह पूरे समाज के भीतर छिपे हुए असंतुलन, दबाव और संवेदनहीनता का दर्पण बन जाती है। हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वाई पूरन कुमार की आत्महत्या ऐसी ही एक घटना है — जो केवल पुलिस विभाग की त्रासदी नहीं, बल्कि उस मानसिक, प्रशासनिक और सामाजिक ढाँचे की विफलता का प्रतीक है, जिसमें पद और प्रतिष्ठा के बावजूद इंसान अकेला और असहाय महसूस करने लगता है।
पूरन कुमार का शव चंडीगढ़ स्थित उनके घर के तहखाने में मिला, जहाँ बताया गया कि वह कमरा पूरी तरह ध्वनि-रोधक था। उनके पास से सरकारी पिस्तौल बरामद हुई। उनकी पत्नी अमनीत कौर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं, जो उस समय जापान में थीं। कोई आत्महत्या-पत्र नहीं मिला। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि पूरा प्रदेश और प्रशासनिक तंत्र स्तब्ध रह गया।
जब कोई पुलिस अधिकारी आत्महत्या करता है, समाज का पहला सवाल होता है – “इतने ऊँचे पद पर था, उसे क्या कमी थी?” यही सवाल हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम यह भूल जाते हैं कि पद, पैसा या अधिकार कभी भी मन की शांति की गारंटी नहीं देते।
प्रत्येक अधिकारी, चाहे वह किसी भी सेवा में हो, सबसे पहले एक मनुष्य होता है। दिन-रात का तनाव, फाइलों के ढेर, राजनीतिक दबाव, निरंतर आलोचना, और एक ऐसे तंत्र की घुटन जिसमें ईमानदारी को अक्सर कमजोरी समझा जाता है — ये सब किसी भी व्यक्ति को भीतर से तोड़ सकते हैं। पूरन कुमार के मामले में कहा जा रहा है कि वे हाल के दिनों में पदोन्नति नीति और वरिष्ठ अधिकारियों के व्यवहार से असंतुष्ट थे। लेकिन क्या इन कारणों से जीवन समाप्त करना उचित था? नहीं। पर यह भी सच है कि जब कोई व्यवस्था भीतर से सड़ जाती है, तो उसमें संवेदनशील और आत्मसम्मानी व्यक्ति सबसे पहले टूटते हैं।
भारत में मानसिक स्वास्थ्य को आज भी कमजोरी के रूप में देखा जाता है। “मैं थक गया हूँ” या “मुझे किसी से बात करनी है” जैसे वाक्य कहने में भी लोग डरते हैं कि कहीं उनकी योग्यता या क्षमता पर प्रश्न न उठ जाए। पुलिस बलों में यह स्थिति और भी गंभीर है। लंबे कार्य घंटे, पारिवारिक जीवन में कमी, जनता और राजनीतिक दबाव, भ्रष्टाचार से जूझना, और ऊँचे अधिकारियों की मनमानी — ये सब मिलकर मानसिक थकान को बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़े बताते हैं कि हर वर्ष सैकड़ों पुलिसकर्मी आत्महत्या करते हैं, लेकिन शायद ही किसी ने यह गंभीरता से पूछा कि क्यों। उनके लिए न तो परामर्श प्रणाली है, न मनोवैज्ञानिक सहायता, न ही सहानुभूति। पूरन कुमार की घटना भी इसी मौन अवसाद का परिणाम प्रतीत होती है।
जब यह ख़बर सामने आई कि “एडीजीपी ने खुद को गोली मारी”, तो सोशल मीडिया पर तरह-तरह की टिप्पणियाँ आने लगीं — “भ्रष्टाचार होगा”, “पारिवारिक विवाद रहा होगा”, “कोई साजिश होगी।” यही हमारी सामाजिक बीमारी है — हम संवेदना से पहले संदेह खोजते हैं। कोई यह नहीं पूछता कि वह व्यक्ति अपने भीतर क्या झेल रहा था। कोई नहीं सोचता कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके सहकर्मी किस पीड़ा से गुजर रहे होंगे। हम केवल सुर्खियाँ बनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए अब मनुष्य नहीं, केवल समाचार बचा है।
एक अधिकारी, जिसने अपना पूरा जीवन कानून और जनता की सेवा में लगाया, अगर उसी व्यवस्था से हारकर जीवन त्याग देता है, तो यह केवल उसकी नहीं बल्कि पूरे तंत्र की आत्महत्या है। यह असफलता उस व्यवस्था की है जो अपने लोगों को भावनात्मक सहारा नहीं दे पाती। यह विफलता उस समाज की है जो केवल सफलता की दौड़ में भागता है, पर सहानुभूति और संतुलन को भूल गया है। और यह शर्म उस मीडिया की है जो किसी की मृत्यु में भी आकर्षण और टीआरपी खोज लेती है। पूरन कुमार की मौत हमसे यह सवाल पूछती है — “क्या इस देश में किसी अधिकारी को ईमानदार, असहमति रखने वाला और संवेदनशील रहकर भी जीने दिया जाएगा?”
देश में प्रशासनिक अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव कोई नई बात नहीं है। फाइलों, तबादलों, पदोन्नतियों और जांचों का जाल इस कदर फैल गया है कि सच्चा और स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हमेशा अकेला पड़ जाता है। पूरन कुमार जैसे अधिकारी, जिनकी पहचान स्पष्टवादिता से थी, अक्सर इसी जाल में फँस जाते हैं। वे न तो झुक पाते हैं, न ही समर्थन पा पाते हैं। परिणामस्वरूप भीतर का अकेलापन उन्हें धीरे-धीरे तोड़ देता है। वर्दी बाहर से चमकती है, पर अंदर का मन बुझ जाता है।
अगर हम सचमुच इस घटना से कुछ सीखना चाहते हैं, तो तीन मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, मानसिक स्वास्थ्य को संस्थागत व्यवस्था का हिस्सा बनाना होगा। हर राज्य में पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के लिए नियमित परामर्श, तनाव प्रबंधन कार्यशालाएँ और गोपनीय सहायता केंद्र होने चाहिए। दूसरा, संवाद और मानवता का वातावरण बनाना होगा। वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों से केवल आदेश नहीं, बल्कि सहानुभूति भी साझा करें। “आप कैसे हैं?” जैसे कुछ शब्द कई बार जीवन बचा सकते हैं। और तीसरा, मीडिया को अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभानी होगी। किसी आत्महत्या की खबर को सनसनीखेज़ बनाना न केवल असंवेदनशील है बल्कि यह समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। समाचारों का उद्देश्य सुधार और समझ होना चाहिए, न कि मनोरंजन।
पूरन कुमार का शव जिस ध्वनि-रोधक कक्ष में मिला, वह केवल एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि पूरे तंत्र की स्थिति का प्रतीक है। एक ऐसा कक्ष, जहाँ बाहर की कोई आवाज़ नहीं पहुँचती और भीतर की कोई पुकार बाहर नहीं आती। यह तहखाना हमारे प्रशासनिक ढाँचे का प्रतीक बन गया है — ऊपर से चमकदार, भीतर से मौन और घुटनभरा।
पूरन कुमार का जाना केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का नुकसान है। यह चेतावनी है कि अगर हमने मानसिक स्वास्थ्य, संवेदनशील नेतृत्व और संवाद को प्राथमिकता नहीं दी, तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएँ और बढ़ेंगी। अब यह स्वीकार करना ही होगा कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक सहयोग किसी भी आधुनिक शासन की उतनी ही आवश्यकता हैं, जितना अनुशासन और उत्तरदायित्व। एक संवेदनशील व्यवस्था ही एक सुरक्षित समाज की नींव रख सकती है।
पूरन कुमार की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके मौन से सबक लें और भविष्य में किसी भी वर्दीधारी को इतना अकेला न होने दें कि वह अपनी ही आवाज़ को बन्दूक से सदा के लिए मौन कर दे।
 “जब वर्दी का बोझ इंसानियत को कुचल दे,
“जब वर्दी का बोझ इंसानियत को कुचल दे,
तो सत्ता नहीं, संवेदना की ज़रूरत होती है।”
-प्रियंका सौरभ
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,